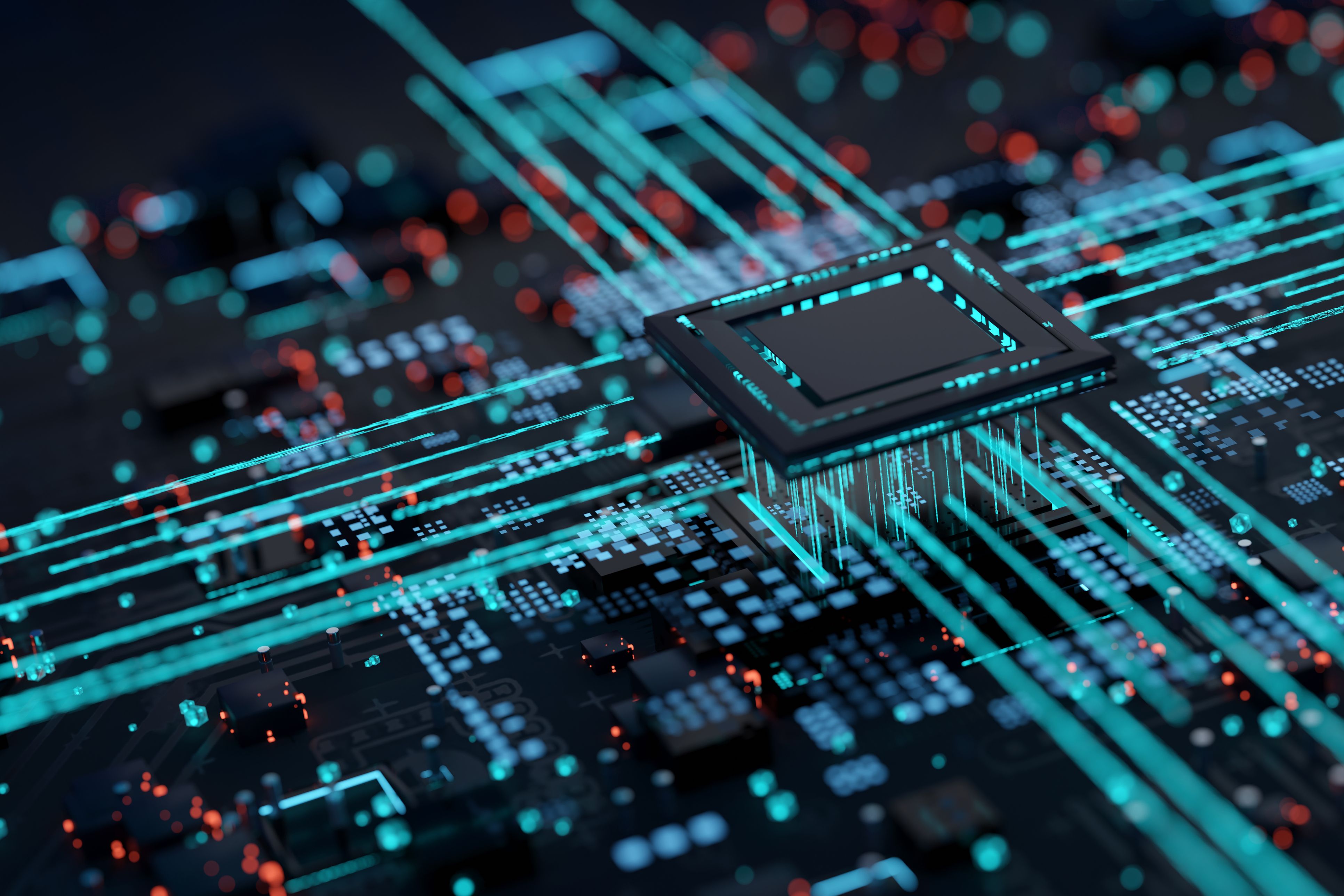टेक-फर्स्ट इंडिया का निर्माण
मोदी सरकार ने पिछले दस साल में कई सुधार किए हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया जितना बदलाव किसी और से नहीं आया।1 जुलाई 2015 में भारत के नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम ने आधार, यूपीआई, ई-साइन और सरकारी ई मार्केटप्लेस जैसे नए कार्यक्रमों के साथ देश को आगे बढ़ाया है।2 इन पहलों ने भारत में क्रांति ला दी है, यहां तक कि देश की गरीब और कम साक्षर आबादी के बीच भी ये कार्यक्रम लगभग पूरे तौर पर लागू हो चुके हैं।
"टेक-फर्स्ट" भारत बनाने में सरकार की भूमिका सबसे अहम है। इस डिजिटल क्रांति की अगुवाई इंडिया स्टैक के ज़रिए की गई , जो हज़ारों पब्लिक और प्राइवेट एप्लिकेशंस का सपोर्ट करने वाला एक ओपन एपीआई-आधारित पब्लिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसने भारत को सबसे विकसित देशों से भी तेज़ रफ्तार दी है।3 हालांकि, तेज़ी से बदल रहे डिजिटल परिदृश्य में, पिछली कामयाबियां ज़्यादा देर तक नहीं रहती हैं। लीडरशिप बनाए रखने के लिए लगातार इनोवेशन और नए हालातों से एडजस्टमेंट ज़रूरी है। इस लेख में, मैं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और पहलों का मूल्यांकन करूंगा, नीतिगत सुधारों और संस्थागत बदलावों के सुझाव दूंगा जो AI की क्षमता का फायदा उठाने, साइबर सुरक्षा को बेहतर करने और साइबर फोरेंसिक विकसित करने के लिए ज़रूरत हैं। इनके अलावा डेटा वेल्थ के रणनीतिक इस्तेमाल, डिजिटल प्रतिस्पर्धा के बीच रास्ता निकालने और क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से उभरती चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। हर सेक्शन में यह जानकारी दी जाएगी कि भारत इन क्षेत्रों में वैश्विक नेता के रूप में कैसे खुद को स्थापित कर सकता है, और लगातार इनोवेशन और आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सकता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
मार्च 2024 में 10,371 करोड़ रुपए (लगभग 1.2 बिलियन डॉलर) के बजट के साथ मंजूर इंडियाएआई मिशन, भारत के डिजिटल सफर में एक बड़ा और सक्रिय कदम है। इसके सात पिलर्स के दायरे में काफ़ी बड़ा क्षेत्र आ जाता है: पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में 10,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) कंप्यूट क्षमता विकसित करना; स्वदेशी डोमेन-स्पेसिफिक बड़े मल्टीमॉडल मॉडलों का विकास; युनिफाइड डेटा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना; AI एप्लिकेशंस के विकास के लिए इंडस्ट्री को फंड देना; AI स्किल्स में मानव संसाधन का विकास; स्टार्टअप्स को डीप टेक AI फंडिंग; और सुरक्षित और एथिकल AI को बढ़ावा देना।4
इंडियाएआई मिशन के तहत प्रस्तावित 10,000 GPU चीन और अमेरिका जैसे इंडस्ट्री लीडरों के मुकाबले मामूली हैं, जिन्होंने पिछले एक दशक में आक्रामक तरीके से GPU हासिल किए हैं और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। हालांकि, भारत को GPU की तादाद में उनकी बराबरी करने या उनसे आगे निकलने की कोशिश करके उनकी रणनीति की नकल करने की ज़रूरत नहीं है।5 इसके बजाय, उसे एक स्मार्ट फ़ास्ट फॉलोअर का नज़रिया रखना चाहिए। हमारे मुताबिक इस नज़रिये की कुछ खासियतें हैं।
सबसे पहले, अपने 10,000 GPU के लिए वेंडर्स को सूचीबद्ध करने से सरकार को तेज़, कम लागत वाले तरीके से हाई-क्वालिटी वाली कंप्यूट फेसिलिटी तैयार करने और GPU के लिए एक बड़ा बाज़ार बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि, संभावित दिक्कतों जैसे काम का लगातार चलना, वेंडर लॉक-इन और डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का हल निकालना होगा। इसके बाद, भारतीय स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों के लिए सुलभ हो जो प्रति GPU घंटे 100 रुपए (लगभग $1.20) की मौजूदा बाज़ार कीमत नहीं दे सकते।6 इमर्जिंग स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी एक सही तरीका हो सकता है। तीसरा, सरकार को कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जल और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर कंप्यूट क्षमता को निर्देशित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, और आधारभूत मॉडलों पर फोकस करना चाहिए।
चौथा, सॉवरेन AI विकास को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक और सुरक्षा डोमेन को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सॉवरेन AI की ज़रूरत वैश्विक संदर्भ से भी मज़बूत होती है - 2020 में, अमेरिका ने क्लीन नेटवर्क इनीशिएटिव लॉन्च किया, जिसके निशाने पर चीनी क्लाउड प्रोवाइडर्स थे, जबकि कई यूरोपीय देशों में उन पर नज़र रखे जाने के डर से अमेरिकी क्लाउड सर्विसेज़ को लेकर तेज़ी से संदेह बढ़ा है।7 इस वजह से क्लाउड सर्टिफिकेशन स्कीम्स सामने आई हैं जो कुछ खास प्रोवाइडर्स को विशेष सरकारी संगठनों को सर्विस देने से रोकती हैं।8 इसके बावजूद, AI के लिए कंप्यूट फिलहाल चीन और अमेरिका के हाइपरस्केलर्स के दबदबे वाले क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। एक स्टडी से पता चलता है कि यूएस की अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और गूगल क्लाउड सामूहिक रूप से ग्लोबल पब्लिक क्लाउड बाज़ार के करीब 70 प्रतिशत पर कब्जा रखते हैं, जबकि बचे हिस्से के ज़्यादातर पर चीनी तकनीकी दिग्गज अलीबाबा, हुआवेई और टेनसेंट का कंट्रोल है।9
इसलिए, महत्वपूर्ण डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विदेशी क्लाउड सर्विसेज़ पर निर्भरता कम करने के लिए, यह ज़रूरी है कि कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में ही हो और एक भारतीय क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर काम करे। सरकार इस बात पर भी विचार कर सकती है कि कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के एक हिस्से को सुरक्षित, नॉन-क्लाउड एन्वायरनमेंट में रखा जाए, जो खास तौर पर संवेदनशील या क्लासिफ़ाइड एप्लिकेशंस के लिए बनाया गया हो। पांचवां, पेशेवर विशेषज्ञता वाले इंडस्ट्री लीडरों और सरकार के प्रतिनिधियों की अगुवाई में एक ऑटोनोमस बॉडी को इस तरह की फेसिलिटी का मैनेजमेंट करना चाहिए, काफ़ी कुछ IN-SPACe मॉडल की तरह।10 छठा, भारत मौजूदा बड़ी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या पारंपरिक कंप्यूटरों से कंप्यूट क्षमताओं का फायदा उठाने के लिए ओपन क्लाउड कंप्यूट प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है।11
सातवां, भारत को अपने डोमेन-स्पेसिफिक डेटा की ताक़त का फायदा उठाने की ज़रूरत है। भारत उन देशों में एक है, जहां दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, और इस वजह से भारत के डेटा में जीवंतता और विविधता है, जो AI मॉडल विकास के लिए ज़रूरी है। इस डेटासेट को स्टार्टअप और इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध कराकर, हम भारत और बाकी दुनिया के लिए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में कॉन्टेक्स्ट-स्पेसिफिक फाउंडेशनल मॉडल और AI एप्लिकेशंस विकसित कर सकते हैं। AI मॉडलों की ट्रेनिंग के लिए डिजिटल एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (DEPA) फ्रेमवर्क के ज़रिए डेटा साझा करने का स्केलेबल और ओपन API सिस्टम एक मजबूत ढांचा देता है, जिससे यह पक्का होता है कि हर तरह का डेटा फ्लो कन्सेंट-बेस्ड और सिक्योर है, और उनका सपोर्ट किया जाना चाहिए।12 फाइनेंशियल सेक्टर में अकाउंट एग्रीगेटर (AA) सिस्टम को कामयाबी के साथ लागू करने का कदम - जिसमें 2.12 अरब फाइनेंशियल अकाउंट डेटा साझा कर सकते हैं - स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी दोहराया जाना चाहिए।13
आठवां, भारत को दुनिया भर में 10 करोड़ से ज़्यादा AI नौकरियों की अनुमानित वैश्विक मांग का दस फीसदी हासिल करने के लिए अपने AI मानव संसाधनों को बढ़ाने की ज़रूरत है।14 इस प्रक्रिया को बाज़ार आधारित और इंडस्ट्री की अगुवाई में होना चाहिए क्योंकि इसमें लाखों अन्य लोगों के साथ-साथ मौजूदा कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित करने का काम होगा। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र का विकास मुख्य रूप से इंडस्ट्री की अगुवाई में हुआ था। जैसे-जैसे हुनरमंद मानव संसाधनों की मांग बढ़ती है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ सॉफ़्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़ (NASSCOM) जैसी इंडस्ट्री बॉडी अलग-अलग भूमिकाओं के लिए ज़रूरी हुनर के स्तर की पहचान करके एक अहम काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशंस को तैयार करके प्राइवेट सेक्टर को AI स्किलिंग में भाग लेने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्किलिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बाज़ार-आधारित स्किलिंग मॉडल की ज़रूरत होगी, साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेजों के अलावा भी STEM कॉलेजों में AI स्किलिंग पहुंचाना ज़रूरी होगा, जिससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में नौजवानों को AI से जुड़ी ट्रेनिंग के लिए आकर्षित किया जा सके। नैसकॉम सर्टिफाइड कोर्सेज़ के लिए स्टैंडर्ड्स बना सकता है, जो स्किलिंग सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी स्किल और स्ट्रैटेजी की गहरी स्टडी पर आधारित हो। मुख्य उद्देश्य मांग, शिक्षा और कौशल के बीच एक मजबूत संबंध बनाना है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सटीक एजुकेशन और ट्रेनिंग इनीशिएटिव्स के ज़रिए बाज़ार की ज़रूरतों को असरदार तरीके से पूरा किया जा सके।
आखिरी लेकिन ज़रूरी बात, AI में ज़्यादा भरोसा पैदा करने के लिए, दूरदर्शी कानून ज़रूरी है। दुनिया भर में कई देश ऐसे कानून बना रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का AI एक्ट AI के लिए नियम-आधारित दृष्टिकोण का उदाहरण है, जिसके मुताबिक यह ज़रूरी है कि भागीदार अपने खास दायित्व पूरा करें।15 चीन, ब्राज़ील और कनाडा के कानूनों में यही दृष्टिकोण है। इसके उलट, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और जापान जैसे देशों ने नरम सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण को चुना है जिसमें डेवलपर्स को नियम-कानूनों की व्याख्या करने और जैसा वे उचित समझें, जोखिम कम करने वाले वैसे उपायों को लागू करने की छूट मिलती है।16 AI गवर्नेंस के बारे में भारत की मौजूदा जागरूकता को देखते हुए, नियम-आधारित दृष्टिकोण सही लगता है। हालांकि, असरदार कानून बनाने के लिए भारत के कानूनी ढांचे की गहरी समझ की ज़रूरत है।
इसके अलावा, समाज के अलग-अलग क्षेत्रों पर असर डालने की AI की खासियत इस बात को ज़रूरी बना देती है कि इस पर कानून बनाने वालों को सामाजिक-तकनीकी-कानूनी परिदृश्य की व्यापक समझ हो। इसलिए, एक सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाना, इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए बेहतर होगा। ऐसी लीडरशिप एक संतुलित, निष्पक्ष दृष्टिकोण सुनिश्चित कर सकती है जो हर तरह के हक और ज़रूरतों का ख्याल रखे।
साइबर सिक्योरिटी
डिजिटाइज़ेशन बढ़ने के साथ-साथ साइबर हमलों और साइबर अपराधों ने बड़े आर्थिक नुकसान और गोपनीयता से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा दिया है। साइबर सिक्योरिटी में हल्के-फुल्के इनोवेशन नए उभरते डोमेन से ख़तरों का मुकाबला करने के लिए जूझते दिखते हैं। मौजूदा पब्लिक की (कुंजी) एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, जो एन्क्रिप्शन के लिए एक पब्लिक की (कुंजी) और डिक्रिप्शन के लिए एक प्राइवेट की (कुंजी) का इस्तेमाल करते हैं - अक्सर डिजिटल हस्ताक्षरों को सत्यापित करने के लिए - उसे क्वांटम कंप्यूटिंग से काफ़ी बड़े ख़तरे हैं। इस बीच, हैकर्स नए प्रकार के साइबर हमलों को विकसित करने के लिए AI टूल का फायदा ले रहे हैं। क्रिप्टोकरेंसी-आधारित साइबर अपराध एक चर्चित मुद्दा है, और ड्रोन और ऑटोमोबाइल इसके संभावित निशाने बन रहे हैं। यह समस्या पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में गंभीर है, जो डोमेन-स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस की कमी से बढ़ गई है।
रेगुलेशंस यह पक्का करते हैं कि किसी चूक के लिए जवाबदेही और गलत काम के लिए सज़ा तय हो। अभी, सिर्फ बैंकिंग, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एन्टिटीज़ के लिए ऐसे रेगुलेशंस हैं। लेकिन तेल और गैस, मैरिटाइम, स्टील, हेल्थकेयर, शिक्षा, ड्रोन और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर असुरक्षित हैं। खराब कोडिंग स्टैंडर्ड और स्किल्ड मैनपावर की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है। कोडिंग में स्किलिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की तरफ से 2014 में मंजूर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एकेडमीज़ एक सराहनीय पहल थी, जिसका मकसद टियर-2 और 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों के 92,800 शिक्षकों को ट्रेनिंग देना था।17 ऐसे और प्रोग्राम लागू किए जाने चाहिए। साथ ही, यह ज़रूरी है कि नैसकॉम जैसी इंडस्ट्री बॉडी बाज़ार की मांग के मुताबिक स्किलिंग स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करने के लिए ऐसे प्रोग्राम तैयार करने में शामिल की जाएं। ऐसे स्टैंडर्ड्स की अतिरिक्त समीक्षा सेक्टर स्किल काउंसिल कर सकती है।
2013 के संस्करण की जगह लेने के लिए एक नई साइबर सुरक्षा नीति का लंबे वक्त से इंतज़ार है, न केवल नए शब्दों के साथ बल्कि पहले से काफ़ी अलग आज की साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक दूरदर्शी रणनीति के साथ भी। इस नीति का मकसद देश भर के संस्थानों, विशेष रूप से उन संस्थानों को गाइड करने का होना चाहिए जो साइबर सुरक्षा खतरों और उनके समाधान के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। इसके लिए, ड्रोन और ऑटोमोबाइल समेत सभी अहम सेक्टरों के लिए सेक्टर-स्पेसिफिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और निगरानी को साइबर सुरक्षा के सभी उभरते क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ विकसित किया जाना चाहिए। फेडरल एजेंसियों के लिए अमेरिका के मैंडेट को उदाहरण मानते हुए, क्रिटिकल एप्लिकेशंस के लिए पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) सॉल्यूशन्स की तरफ जाने का एक रोडमैप तैयार करना चाहिए।18 घरेलू ज़रूरतों और एक्सपोर्ट में विशेषज्ञता को पूरा करने के लिए साइबर सुरक्षा से जुड़ा मानव संसाधन विकास बेहद अहम है। MeitY के स्किलिंग इनीशिएटिव को ज़्यादा फंड के साथ बढ़ावा देना चाहिए और देश भर में और ज़्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजों तक ले जाया जाना चाहिए, इसमें ऑनलाइन स्किलिंग प्लेटफ़ॉर्म को भी शामिल करना चाहिए। न सिर्फ आईटी सेक्टर में, बल्कि दूसरे सेक्टरों में भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनलों की बढ़ती मांग को देखते हुए, MeitY के लिए डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाना ज़रूरी हो जाता है जो गैर-आईटी उद्योग के यूज़र्स की ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के संपर्क में लाए।
साइबर फोरेंसिक
मौजूदा डिजिटल दौर में, इंटरनेट पर हर एक्शन एक डिजिटल निशान छोड़ता है जो एनालिसिस और जांच के दायरे में होता है। डिजिटल फोरेंसिक बाज़ार सालाना 16.3 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।19 भारत में, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, डेटा फ़िड्युसरी (डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या संस्थान) को कानूनी जिम्मेदारी दी गई है, जिससे इस बाज़ार को काफी बढ़ावा मिल रहा है।20 एक बेहतर आईटी इंडस्ट्री के बावजूद, भारत इंपोर्टेड टूल्स पर निर्भर है और यहां स्किल्ड मैनपावर की कमी है। चुनिंदा पुलिस और जांच एजेंसियों को डिजिटल फोरेंसिक में ट्रेनिंग दी जाती है- यह खालीपन कारोबार तक में दिखता है। एक तरफ जहां प्राइवेट सेक्टर से डिजिटल फोरेंसिक सर्विसेज़ और एप्लिकेशंस की तैयारियों में नेतृत्व करने की उम्मीद है, वहीं पुलिस बलों और संबंधित सरकारी विभागों को अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करने लायक बनने के लिए सही ढंग से ट्रेनिंग लेनी होगी। फोरेंसिक क्षमताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पुलिस अफसरों के लिए सही ट्रेनिंग पक्का करना ज़रूरी है। सरकार को, देश में अपनी तरह की पहली, गुजरात की नेशनल फोरेंसिक साइंसेज़ यूनिवर्सिटी को मिसाल मानते हुए बुनियादी ढांचा तैयार करने और बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इस फ़ील्ड में कोर्सेज़ तैयार करने और उनकी पढ़ाई कराने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अभी, सिर्फ सरकारी प्रयोगशालाओं को आईटी एक्ट, 2008 के तहत "इलेक्ट्रॉनिक सबूत के जांचकर्ता" के तौर पर नोटिफ़ाई किया जा सकता है।21 सरकार को सेक्शन 79ए के तहत निजी प्रयोगशालाओं को नोटिफ़ाई करना चाहिए, पुलिस, प्रॉसिक्यूटर और ज्युडिशियरी के लिए ट्रेनिंग शुरू करना चाहिए और फोरेंसिक टूल्स के लिए स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च करने चाहिए। MeitY को इन टूल्स के लिए भारतीय मानक विकसित करने चाहिए, और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को बैंकिंग और फ़ार्मा जैसे जोखिम वाले सेक्टरों में डिजिटल फोरेंसिक के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रसिजर्स (SOP) बनानी चाहिए।
डेटा वेल्थ का इस्तेमाल करना
गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॅन जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियां डेटा का फायदा उठाकर ट्रिलियन डॉलर की कंपनियां बन गई हैं। दुनिया के सबसे बड़े डेटा प्रोड्यूसरों में से एक के रूप में, भारत में इतनी क्षमता है कि वो डेटा मॉनेटाइज़ेशन मॉडलों की मदद से अपनी जीडीपी में अहम योगदान कर सकता है, और इससे यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि लोग अपने डेटा का भी फायदा उठा पाएं। AA सिस्टम यूज़र्स को अपनी वित्तीय जानकारी को संस्थानों के साथ सुरक्षित रूप से साझा करने का हक देता है, जिससे गोपनीयता बनाए रखते हुए लोन, इन्वेस्टमेंट और दूसरी चीज़ों पर बेहतर डील मिल सकती है। डेटाएम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर(DEPA) के साथ-साथ AA सिस्टम के भीतर किए गए काम को स्वास्थ्य, फ़ार्मा और शिक्षा समेत बाकी सेक्टरों में डेटा मॉनेटाइज़ेशन के लायक बनाने के लिए पूरी इकॉनमी में लागू किया जाना चाहिए।
ज़मीन और ज़मीन के किसी हिस्से से जुड़ी जानकारी जीडीपी की सालाना बढ़ोतरी में 0.5 प्रतिशत का योगदान दे सकती है, फिर भी भारत में ज़मीन की स्थानीय जानकारी देने वाले अच्छे क्वालिटी के डेटा की कमी बनी हुई है। स्वामित्व योजना, जिसमें ड्रोन सर्वे का इस्तेमाल होता है, को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिनका हल निकाला जाना चाहिए।22 फरवरी 2021 में मैप पॉलिसी में हुए सुधार और अगस्त 2021 में नई ड्रोन नीति जियोस्पेशल डेटा में सुधार की बुनियाद रखती है। इस दिशा में अगला अहम कदम देश भर के जियोस्पेशल डेटा को तेज़ी से इकट्ठा करना हो सकता है। जियोग्राफ़िक इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS) पर आधारित नेशनल मास्टर प्लान- पीएम गतिशक्ति बुनियादी ढांचे में निवेश की कार्यकुशलता बढ़ाने वाला प्लान है और इसे सभी प्रोजेक्ट्स के लिए लागू किया जाना चाहिए।23 पानी के नीचे के इलाकों के लिए पीएम गतिशक्ति इनीशिएटिव, स्मार्ट सिटीज़ की तरह स्मार्ट समुद्री इलाकों को विकसित करके, टेक्नोलॉजी-ड्रिवन मैरिटाइम स्पेशल प्लानिंग में मदद कर सकता है जिससे ब्लू इकॉनमी के आर्थिक फ़ायदे मिल सकते हैं। इससे समुद्री संसाधनों का उचित और लंबे समय तक चलने वाला दोहन सुनिश्चित होगा और जलमार्गों में सुरक्षित परिवहन, खोजबीन और रिकवरी के काम, आर्थिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा और पानी के नीचे प्रदूषण की रोकथाम जैसी चुनौतियों का हल मिलेगा।
“मेक इन इंडिया” से “मेक प्रोडक्ट्स इन इंडिया” की तरफ कदम
टेक्नोलॉजी पर आधारित नॉलेज इकॉनमी में, किसी प्रोडक्ट की बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) उसकी कुल कीमत का आधा या उससे भी ज़्यादा होती है, जिससे अकेले मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए वैल्यू-क्रिएशन को एक बराबर करना चुनौती भरा हो जाता है। इसे समझते हुए चीन ने अपना ध्यान ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब होने से हटाकर 2050 तक इनोवेशन में वर्ल्ड लीडर बनने पर लगा दिया है। भारत को एक “विकसित” देश बनने के लिए, उसे “मेक इन इंडिया” से “मेक प्रोडक्ट्स इन इंडिया” का रास्ता तय करना होगा, ताकि मिडिल-इनकम के फंदे में फंसने या अमीर बनने से पहले बूढ़े होने के जोखिम से बचा जा सके। हालांकि भारत आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड सर्विसेज (ITeS) में अच्छा कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और प्रोत्साहनों में सुधार की तुरंत ज़रूरत है। ध्यान उस जगह केंद्रित होना चाहिए जहां असली वैल्यू है: IP और प्रौद्योगिकी का विकास, खास तौर पर डिजिटल डोमेन में, जहां IP कुल कीमत का लगभग 50 प्रतिशत या उससे ज़्यादा हो सकता है। IP को नियंत्रित करने से न केवल आर्थिक फायदे होते हैं बल्कि रणनीतिक फायदे भी मिलते हैं।
साथ ही, "मेक इन इंडिया" के तहत मैन्युफैक्चरिंग में लगातार कोशिशें रोज़गार पैदा करने के लिए अहम होंगी, खासकर देश की नौजवान आबादी को देखते हुए। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक मज़बूत बुनियाद बनाता है, लेकिन और ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत है। इसका मंत्र होना चाहिए "ईज़-ऑफ-डूइंग इनोवेशन", जिसमें लिखे हुए नियमों और प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू करने के मुकाबले इनोवेशन की ख़ूबियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इनोवेटर्स के लिए सरकारी खरीद को बढ़ावा देकर ना सिर्फ उन्हें एक पहचान दी जा सकती है, बल्कि कंज़्यूमर के भरोसे को बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए रेवेन्यू का एक ज़रिया भी पक्का किया जा सकता है। जनरल फ़ाइनेंशियल रूल्स (GFR) में एक साफ़ फ्रेमवर्क तैयार करने की ज़रूरत है ताकि अपने देश में बने प्रोडक्ट्स की परिभाषा सही ढंग से तय हो, साथ ही कीमतें तय करने के लिए एक सिस्टम भी।
सरकार को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जोखिम कम करने के लिए आर्थिक मदद करनी चाहिए, खास तौर पर फैबलेस चिप डिज़ाइन में, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स की बुनियाद है। अमेरिका में डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी (DARPA) और इज़राइल में योज़मा जैसे कामयाब मॉडलों से इसके लिए गहरी समझ मिल सकती है।24 द इनोवेशन्स फॉर डिफेंस एक्सलेस (iDEX) मॉडल का दायरा रक्षा क्षेत्र से आगे ले जाना चाहिए। ये मॉडल ऐसा इकोसिस्टम तैयार करता है जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के साथ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ (MSMEs), स्टार्टअप, इनोवेटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) इंस्टीट्यूट्स और शिक्षाविद जुड़ते हैं।25 अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने iDEX लॉन्च किया था, और बड़े बदलाव लाने वाली इस पहल ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (DISC) के ज़रिए डिफेंस इनोवेशन को बढ़ावा दिया।26 सेना, नौसेना और वायु सेना की खास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्टार्टअप को मौका देकर iDEX ने तेज़ी से अपने देश में ही टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस तैयार कराए। 1.5 करोड़ रुपए (करीब 180,000 डॉलर) तक की मदद के साथ, स्टार्टअप ने बारह से अठारह महीनों में कम लागत और अच्छी क्वालिटी वाले इनोवेशंस डेवलप किए, जिसने भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में बड़े बदलाव ला दिए। पिछले नियमों से हटकर, iDEX ने स्टार्टअप को अनुमति दी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) राइट्स वो रख सकते हैं, हालांकि सरकार ने राष्ट्रीय हित के लिए मार्च-इन राइट्स अपने पास रखे। इस प्रोजेक्ट ने स्टार्टअप्स को कमर्शियल और एक्सपोर्ट के मौके तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। iDEX मॉडल का दायरा बढ़ाने के अलावा, बढ़ी हुई सरकारी भागीदारी के साथ आरएंडडी-फोकस्ड फंड की शुरुआत करने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है और इनोवेशन से जुड़े जोखिम असरदार ढंग से कम किए जा सकते हैं।
भारत के डेमोग्राफिक फायदे को AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन जैसी तेज़ी से बढ़ रही प्रौद्योगिकियों में टैलेंट पूल के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कामयाबी से सीख लेते हुए, भारत में एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ को एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के सेंटर के तौर पर काम करना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया इनीशिएटिव ने असाधारण तरक्की की है, जिसके तहत देश भर में कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज सरकारी मदद से स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं।27अगला महत्वपूर्ण कदम वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री का विस्तार करना और इन इनक्यूबेटरों के साथ कनेक्शन बनाना है। हाल ही में लॉन्च किए गए माउंटटेक ग्रोथ फंड ने रक्षा, अंतरिक्ष और डीप टेक पर फोकस किया है, जिसने तकनीकी उद्यमों के लिए रिस्क फंडिंग मुहैया कराने के लिए कई कॉलेज इनक्यूबेटरों के साथ मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) किए हैं।28 इसके अलावा प्रयोगशाला में हो रहे रिसर्च को कामयाब कमर्शियल एंटरप्राइज़ में बदले जाने की क्षमता को एकेडमिक फैकल्टी के मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण मापदंड बनाया जाना चाहिए। राज्य सरकारें अपनी यूनिवर्सिटीज़ की इनक्यूबेशन गतिविधियों के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम्स को जोड़कर एक सपोर्टिव इकोसिस्टम बना सकती हैं।
इंटेल, सैमसंग और एप्पल जैसे ग्लोबल ब्रांड के दबदबे को चुनौती देने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों के लिए एक ब्रांड बनाना और लोगों में उसके प्रति भरोसा जमाना ज़रूरी है। देश के अपने इनोवेशन को दुनिया भर में पहचान दिलाने का काम इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) को सौंपा जा सकता है।29 स्वदेशी उत्पादों में भरोसा पैदा करने का एक उल्लेखनीय उदाहरण कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के स्वदेशी टीके कोवैक्सिन को कमतर आंकने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सबसे पहले इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया।30 इस तरह सार्वजनिक तौर पर समर्थन देने से ब्रांड की पहचान और विश्वसनीयता काफ़ी बढ़ती है। इसके अलावा, अपनी नीति के रूप में, सरकार को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चैनलों के ज़रिए स्वदेश में विकसित उत्पादों के एक्सपोर्ट को ज़ोर-शोर से बढ़ावा देना चाहिए। जहां भी मुमकिन हो, इन देशी उत्पादों को बांटे जाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी स्वीकृति बढ़े।
टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और उन्हें अपनाने के लिए स्टैंडर्ड तैयार करने की अहमियत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। स्टैंडर्ड्स यूनिफ़ाइड मार्केट बनाने, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ उनकी लागत कम करने, और दुनिया भर में इनोवेशंस को मान्यता दिलाने में मदद करते हैं। 2012 में MeitY का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत वाला ऑर्डर भारी-भरकम लाइसेंस-बेस्ड सिस्टम की जगह सेल्फ़-रजिस्ट्रेशन शुरू करके स्टैंडर्ड्स को लागू करने में एक बड़ी कामयाबी थी।31 इस वजह से 2016 में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम में संशोधन हुए, जिससे सेल्फ़-रजिस्ट्रेशन और सेल्फ़-सर्टिफ़िकेशन की लोकप्रियता बढ़ गई। नतीजतन, स्टैंडर्ड्स अपनाने की तादाद 2014 में बहुत थोड़े से बढ़कर 2023 तक 500 से ज़्यादा हो गई, और उम्मीद है कि जल्द ही करीब 2,000 और जुड़ जाएंगे।32
उभरती डिजिटल तकनीकों के लिए नए मानक विकसित करने की पहल की लीडरशिप MeitY को लेनी चाहिए। एक बार जब भारत इन नई क्षमताओं, तरीकों या उत्पादों के लिए अपने मानक बना लेता है, तो MeitY को इन मानकों को दुनिया भर में मान्यता दिलाने की दिशा में भी काम करना चाहिए। डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ के लिए बड़ा भारतीय बाज़ार इस कोशिश में मदद कर सकता है। इंडिया स्टैक, जो एक राष्ट्रीय मानक के तौर पर शुरू हुआ और बाद में दुनिया भर में पहचाना गया, उसकी कामयाबी को इस सेक्टर में आने वाले इनोवेशंस के लिए दोहराया जाना चाहिए।” अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाने वाली संस्थाओं में फ़ैसले लेने वाली भूमिकाओं तक पहुंचने के लिए सरकार और उद्योग का साथ ज़रूरी है। अलग-अलग तकनीकी क्षेत्रों में राष्ट्रीय मानक बनाने वाली संस्थाएं उद्योगों के नेतृत्व में हो सकती हैं, जिसमें शुरुआती कदम के तौर पर इन संस्थाओं को कानूनी मान्यता दी जा सकती है।
डिजिटल मुक़ाबले से निपटना
डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ में अक्सर मज़बूत नेटवर्क का असर दिखता है और सिर्फ़ विनर कंपनी की पूछ होती है, जिससे बाज़ार पर किसी एक कंपनी या कंपनियों के छोटे ग्रुप का कब्ज़ा हो जाता है, जैसे गूगल सर्च, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट्सऐप, और फ़ेसबुक। डिजिटलाइज़ेशन ने जीडीपी में नेटवर्क इकॉनमी की हिस्सेदारी काफ़ी बढ़ा दी है, और इस ट्रेंड के आगे और बढ़ने की उम्मीद है। डिजिटल डोमेन में प्रतिस्पर्धा की समस्या का समाधान करना सरकारों और रेगुलेटरों के लिए एक मुश्किल चुनौती है। जैसे-जैसे नेटवर्क का दायरा बढ़ता है और यूज़र्स की तादाद बढ़ती जाती है, नेटवर्क के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ पब्लिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ की शक्ल लेने लगते हैं, हालांकि उनका कंट्रोल प्राइवेट हाथों में रहता है जिससे पॉलिसीज़ पर काफ़ी असर पड़ता है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से अनुमान लगाकर किए जाए वाले नियंत्रण (ex-ante control) के साथ एक ड्राफ्ट कानून की सिफारिश की है। इन चुनौतियों में शामिल है मौजूदा नेटवर्क में प्रोडक्ट्स को बंडल करना या जोड़ना, ख़ुद को तरजीह देना, तीसरे पक्ष के प्रोडक्ट्स को रोकना, डेटा पर एकाधिकार, ई-कॉमर्स पर भारी छूट, एक्सक्लूसिव टाई-अप्स, सर्च एंड रैंकिंग में प्राथमिकता तय करना, तीसरे पक्ष के ऐप पर रोक लगाना और प्रतिस्पर्धा-विरोधी विज्ञापन नीतियां।33
हालांकि, ऐसे रेगुलेशन के प्रस्ताव से ये चिंताएं पैदा होती हैं कि ऐसे रेगुलेशन का माहौल लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज जैसा हो सकता है, जो शायद इस सेक्टर की खासियत रही इनोवेटिव फ्रीडम को सीमित कर दे। पिछले अनुभवों से पता चलता है कि ऐसे रेगुलेशन अक्सर नेटवर्क प्रोडक्ट्स में मोनोपली या ओलिगोपली को रोकने में नाकाम रहे हैं, जैसा कि टेलीफ़ोनी में देखा गया है, जहां फ्रांस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देशों में ऐसे रेगुलेशन्स के बावजूद मोनोपली के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा, पहले से अनुमान लगाकर किए जाए वाले नियंत्रण इनोवेशन को धीमा कर सकते हैं, क्योंकि कीमतों पर नियंत्रण लगाने की प्रक्रिया बाज़ार में पहले से मौजूद खिलाड़ियों को तय रिटर्न देती है, और ये खिलाड़ी फिर रेगुलेशन मानने की आड़ में नए खिलाड़ियों की एंट्री के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं।
हालांकि इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इंटरनेट की ग्रोथ से सबक सीखा जा सकता है - मोनोपली होने के बावजूद, इसने इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हुए कंज़्यूमर की भलाई सुनिश्चित करने में कामयाबी हासिल की है। सरकार नेटवर्क इकॉनमी प्रोडक्ट्स को नियंत्रित करने के लिए कानूनी मेकेनिज़्म बना सकती है, जिससे यह पक्का हो सके कि सभी स्टेकहोल्डर एक जैसे स्तर पर हों। सरकार का किसी मामले में सीधा हल निश्चित करने से दूर रहना बेहतर है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के मामलों में फ़ैसले की ताक़त को अपने पास रख सकती है। बड़े बदलाव लाने के काबिल इस आर्थिक घटना से असरदार ढंग से निपटने के लिए एक अलग सोच की ज़रूरत होगी।
क्वांटम कंप्यूटिंग
क्वांटम कंप्यूटिंग (QC) के आने के साथ क्लासिकल डिजिटल दुनिया में हलचल मच गई है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग उन समस्याओं को कुछ मिनट में हल कर सकता है, जिसके लिए एडवांस्ड सुपरकंप्यूटर को भी हज़ारों साल लगेंगे। चीन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश सबसे आगे हैं, और भारत को उनकी बराबरी पर आना होगा। इंडियन नेशनल क्वांटम मिशन (INQM) को कैबिनेट की मंज़ूरी एक बड़ा कदम है, लेकिन इस काम में इंडस्ट्री की ज़्यादा भागीदारी अहम होगी।34 भारत में, QC रिसर्च मुख्य रूप से सरकारी प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर में इस क्षेत्र में तरक्की का काम इंडस्ट्री और स्टार्टअप ने किया है। QC फार्मा, हेल्थकेयर, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, एयरोनॉटिक्स और स्पेस जैसे सेक्टरों में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने में काबिल है। इस पोटेंशियाल का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए, भारत को ऐसी नीतियों की ज़रूरत है जो इंडस्ट्री लीडर्स और स्टार्टअप्स को R&D में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अलावा विकसित हो रहे ज्ञान के साथ तालमेल रखने के मकसद से टेस्टिंग, सर्टिफ़िकेशन और स्टैंडर्ड के लिए इंडस्ट्री की लीडरशिप वाला फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष
भारत की “टेक-फर्स्ट” राष्ट्र बनने की यात्रा महत्वाकांक्षी और प्रेरणादायक दोनों है। डिजिटल इंडिया और AI मिशन जैसी सरकार की रणनीतिक पहल लगातार इनोवेशन और डिजिटल बदलाव के लिए एक मज़बूत बुनियाद देती है। हालांकि, तेज़ी से बदल रहे इस माहौल में आगे रहने के लिए लगातार अपने को ढालने, घरेलू प्रतिभा को बढ़ावा देने और साइबर सुरक्षा उपायों को मज़बूत करने की ज़रूरत है, जिसके लिए सरकार को आगे बढ़कर उचित नीतिगत ढांचा तैयार करना होगा। अपने समृद्ध डेटा संसाधनों का फ़ायदा उठाकर, AI क्षमताओं को बढ़ाकर और स्वदेशी इनोवेशन को बढ़ावा देकर, भारत न केवल एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के तौर पर अपनी हैसियत सुरक्षित कर सकता है, बल्कि अपने सभी नागरिकों को तरक्की और डिजिटल एंपावरमेंट भी दे सकता है - जो दुनिया भर के देशों के लिए एक मॉडल हो।
*लेखक कार्नेगी इंडिया में नॉन-रेसिडेंट स्कॉलर हैं और माउंटटेक ग्रोथ फंड - कवच के फाउंडर और चेयरमैन हैं। लेखक कार्नेगी इंडिया में रिसर्च असिस्टेंट चारुकेशी भट्ट को उनकी मदद के लिए धन्यवाद करते हैं।
भारत में AI: रेगुलेशन या इंतज़ार?
दुनिया भर की सरकारें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) के नियम-कायदों को लागू करने के अलग-अलग चरणों में हैं। यूरोपियन यूनियन इस साल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक्ट लागू करना शुरू कर देगा;1 कनाडा और कैलिफोर्निया के सांसदों ने AI सुरक्षा विधेयक पेश किए हैं, जो अभी तक कानून नहीं बन पाए हैं; इस बीच, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, सिंगापुर और जापान अलग-अलग प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें वॉलटंरी कोड ऑफ कंडक्ट से लेकर खास सेक्टर्स और एप्लिकेशन्स के लिए टार्गेटेड रेगुलेशन्स तक शामिल हैं।2
इस लेख में, हमारा सवाल है कि क्या भारत के लिए नए AI रेगुलेशन्स अपनाने का यह सही वक्त है। अब तक, भारत सरकार ने AI रेगुलेशन पर "स्ट्रैटेजिक गाइडेंस" देने के लिए एक हाई-लेवल कमिटी बनाई है, जबकि AI के विकास और उपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए ऐड हॉक नियम और सलाह जारी करना जारी रखा है।3 आगे जाकर, एक नए डिजिटल इंडिया एक्ट में AI रेगुलेशन को शामिल किए जाने की उम्मीद है, हालांकि बिल की मौजूदा स्थिति साफ़ नहीं है।4
हमारी रिसर्च के मुताबिक इस वक्त भारत में नए AI रेगुलेशन्स लाने की कोई साफ़ वजह नहीं है। इसके बजाय, हमें AI से पैदा होने वाले नए जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने और किसी भी नए रेगुलेशन को अपनाने से पहले यह जानने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में नियम-कायदे की कमी है। इसके अलावा, कुछ खास बाज़ारों की नाकामी की पहचान करने के लिए डायनेमिक AI इकोसिस्टम का सावधानी से अध्ययन करने की ज़रूरत है। अभी के लिए हमारा सुझाव है कि रेगुलेशन के लिए एक अस्थायी दृष्टिकोण रखा जाए और उन क्षेत्रों को सामने लाया जाए जिनमें एडिशनल रिसर्च की ज़रूरत है ताकि उन जानकारी का इस्तेमाल भारत में नीति तैयार करने की प्रक्रिया में हो सके।
AI के जोखिमों को समझना
ऐसे कौन से नए जोखिम हैं, अगर हैं तो, जो खास तौर पर AI से जुड़े हो सकते हैं - एक ऐसी तकनीक जो 1950 के दशक से ही मौजूद है - और जिनके लिए तुरंत रेगुलेशन की ज़रूरत है?5 कुछ लोगों का कहना है कि ChatGPT जैसे जनरेटिव AI एप्लिकेशन्स ने सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और पूर्वाग्रह के जोखिम को बढ़ा दिया है।6 हालांकि, जब भारत में पहले से ही ऐसे ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह के मुद्दों को हल करने के लिए सिस्टम मौजूद हैं, तो क्या नए रेगुलेशन को लागू करने की लागत को सही ठहराया जा सकेगा?7
AI जोखिमों के स्वभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए, “AI के गॉडफादर” योशुआ बेंगियो की लीडरशिप में एक्सपर्ट्स के एक पैनल ने तीन कैटेगरीज़ की पहचान की: (1) दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल, (2) अनपेक्षित नतीजे, और (3) बनावट से जुड़े जोखिम (एक चौथी कैटेगरी के साथ)। हालांकि, जैसा कि अंतरिम रिपोर्ट के लेखक खुद मानते हैं, हर जोखिम का पहले से अनुमान लगाना नामुमकिन है, और इसका सबूत यह है कि हम अभी भी बड़े भाषा मॉडलों और जेनरेटिव AI एप्लिकेशन्स के जोखिमों से जूझ रहे हैं।8 इसलिए, असली सवाल यह है: क्या AI नए या अलग तरह के जोखिम लाता है जिनका हम सही ढंग से अनुमान लगा सकते हैं और जिनके लिए नए रेगुलेशन्स की ज़रूरत हो?
AI के मामले में जोखिम का वर्गीकरण स्थानीय वजहों से भी प्रभावित हो सकता है, जैसे कि AI किस लेवल तक अपनाया गया है, कंज़्यूमर किस हद तक जागरूक हैं और किसी खास क्षेत्र के अधिकार और सांस्कृतिक संवेदनशीलता क्या हैं। जिस तरह से यूरोपीय यूनियन और कनाडा की सरकारों ने AI की कुछ ऐसी कैटेगरीज़ की पहचान की है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा जोखिम है, हमारा सुझाव है कि उसी तरह भारत सरकार किसी भी नए रेगुलेशन को लाने के पहले AI के जोखिमों का सबूत के आधार पर मूल्यांकन करे। ये जोखिम स्थानीय परंपराओं, कानूनी अधिकारों और मूल्यों से जुड़े हो सकते हैं।9
हमारा मानना है कि जब तक असली सबूतों पर आधारित फ्रेमवर्क सामने नहीं आ जाता, तब तक भारत के लिए नए AI रेगुलेशन्स को अपनाना जल्दबाज़ी होगी।
मौजूदा कानूनों में खामियों की पहचान
इस वक्त नए AI नियम-कायदे लागू करना इसलिए भी जल्दबाज़ी हो सकती है, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं है कि भारत में मौजूदा कानून AI के उभरते जोखिमों से निपटने के लिए काफ़ी हैं या नहीं। इसके अलावा, एक जैसे कई कानूनी प्रावधान मुकदमेबाज़ी की तादाद को बढ़ा सकते हैं और पहले से ही बोझ से दबी प्रशासनिक और अदालती व्यवस्था और भी दब सकती है।
इसलिए, हमारा सुझाव है कि मौजूदा संवैधानिक सुरक्षा, क़ानून, नियम, रेगुलेशन्स और दूसरे प्रावधानों - डिजिटल कंटेंट, प्राइवेसी और प्रोडक्ट लायबिलिटी से जुड़े हुए - का पूरा विश्लेषण किया जाए, जो AI विकास और इस्तेमाल पर असर डाल सकते हैं। कुछ मामलों में, पहले से अनुमानित जोखिमों का निपटारा करने के लिए एक मामूली संशोधन से भी काम चल सकता है।10 जैसे, डीपफेक के बढ़ते ख़तरे से निपटने के लिए, सरकार मौजूदा कानूनों को अपडेट कर सकती है या उनकी दोबारा व्याख्या कर सकती है ताकि AI से बनाए गए गैरकानूनी कंटेंट के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को रोका जा सके।11 ये कानून हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (पहले का इंडियन पेनल कोड, 1860)।
हालांकि कुछ जगहों पर डिसरप्शन की अहमियत ज़्यादा हो सकती है। जैसे, कॉपीराइट की सुरक्षा मिले हुए मैटेरियल पर आधारित AI से तैयार कंटेंट की भरमार ने इंडियन कॉपीराइट एक्ट, 1957 की गहरी समीक्षा की स्थिति बना दी है।12 इसी तरह लेबर, डेटा प्रोटेक्शन और कंज़्यूमर प्रोटेक्शन से जुड़े कानूनों का विश्लेषण उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए फायदेमंद होगा जिनमें नए अधिकारों, दायित्वों, अपवादों या स्पष्टीकरणों की ज़रूरत हो सकती है।
बाजार के डायनेमिक्स पर नज़र
एक असरदार रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में AI के जोखिमों को बढ़ाने और कम करने में शामिल अलग-अलग पक्षों की भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया की तरफ से कराई जा रही मार्केट स्टडी, AI वैल्यू चेन में अलग-अलग पक्षों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, उनके आपसी संबंधों और इस इकोसिस्टम के दूसरे भागीदारों पर उनके असर जैसी बातों की निगरानी करके रेगुलेटरों को पूरी जानकारी के साथ सही फ़ैसला लेने में मदद करेंगे।13 इससे यह जानने में भी मदद होगी कि बाज़ार की खास नाकामियों का समाधान निकालने के लिए पहले से अनुमान लगाकर अपना नज़रिया तय किया जाए या नहीं (यह डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल के ड्राफ्ट की वजह से गर्मागर्म बहस का मुद्दा बना हुआ है)।14
बाज़ार की स्टडी तब भी अहम होगी जब सरकार व्यावसायिक रूप से संवेदनशील मामलों में दखल देने की योजना बनाएगी, जैसे कि AI-जनरेटेड कंटेंट को लेकर क्रिएटरों और पब्लिशरों के बीच कमाई का बंटवारा। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर भारत के आईटी मंत्री ने संकेत दिया है कि नया "AI कानून" इस बात का ध्यान रखेगा।15 चूंकि इन मुद्दों का हल आम तौर पर कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए निकाला जाता है, इसलिए सरकार को बाज़ार की नाकामी के पर्याप्त सबूत जुटाने होंगे अगर वो नए नियम-कायदों के ज़रिए इस मामले में दखल देना चाहती है।
इसी तरह, बाज़ार की स्टडी यह तय करने में भी मदद करेगी कि रेगुलेशंस किस पर लागू होने चाहिए और इन्हें लागू करने के लिए सबसे छोटी सीमा क्या होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया के AI सेफ्टी बिल के मुख्य प्रावधान सिर्फ़ एडवांस्ड AI मॉडलों पर लागू होते हैं जिन्हें एक तय सीमा में पूंजी का उपयोग करके तैयार किया गया है;16 चीन के जनरेटिव AI नियम सिर्फ़ उन संस्थाओं पर लागू होते हैं जो कुछ खास तरह के काम करती हैं।17
इसी तरह, भारत के AI रेगुलेशंस, अगर और जब भी पेश किए जाते हैं, तो उन्हें बाज़ार के बदलते डायनेमिक्स की जानकारी रखनी होगी। चूंकि इस तरह के डेटा को इकट्ठा करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, इसलिए हमारा मानना है कि इस वक्त नए रेगुलेशंस को अपनाना जल्दबाज़ी होगी।
निष्कर्ष
किसी भी नए AI रेगुलेशंस को अपनाने से पहले, भारतीय नीति निर्माताओं को अलग-अलग बिंदुओं की पूरी समझ होनी चाहिए: AI की वजह से पैदा हुए अनोखे जोखिम, AI इकोसिस्टम के लगातार बदलते डायनेमिक्स, मौजूदा कानूनी ढांचे में खामियां, और साथ ही ऐसे रेगुलेशंस को लागू करने और उनका पालन कराने की लागत।
इस बुनियादी जानकारी के बिना, नए AI रेगुलेशंस को अपनाना जल्दबाज़ी होगी और इससे ऐसे नतीजे भी आ सकते हैं जो फायदों से कहीं ज़्यादा नुकसान कर देंगे। इस विषय पर चल रही हमारी रिसर्च के मुताबिक हमने पाया है कि इस वक्त भारत में नए AI रेगुलेशंस को साफ़ तौर पर सही ठहराने के लिए ज़रूरी जानकारी की कमी है।
दूसरे शब्दों में, अभी रेगुलेशंस का सही वक्त नहीं है।
भारत में बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम: आगे का रास्ता
पिछले दस साल में, भारत की बायोइकॉनमी तेरह गुना बढ़ी है, जो 2014 में 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 130 बिलियन डॉलर हो गई है, तथा 2030 तक इसके 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।1 इस तरक्की को रफ्तार देने का मुख्य काम प्राइवेट सेक्टर ने किया है, जिसे इसी काम के लिए बनाई गईं रिसर्च लैबोरेट्रीज़, बायोसाइंसेज़ में एकेडमिक एक्सलेंस के सेंटर्स, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायो-इनक्यूबेटरों और इंडस्ट्री की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (BIRAC) की स्थापना जैसे सरकारी कदमों से ताक़त मिली है।2 इस सेक्टर की तरक्की मुख्य रूप से बायोफार्मास्युटिकल सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से हुई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स, बायोथेरेप्यूटिक्स और बायोसिमिलर का प्रोडक्शन शामिल है।3
भारत में मैन्युफैक्चरिंग की कम लागत ग्लोबल बायोफार्मा कंपनियों को आकर्षित करती है जो उत्पादन खर्च घटाना चाहती हैं। भारत के सस्ते वैक्सीन उत्पादन ने इसे डीपीटी (डिप्थीरिया-टेटनस-पर्टसिस) और खसरे के वैक्सीन के बड़े सप्लायर के तौर पर स्थापित किया है।4 कोरोना वायरस महामारी के दौरान, भारत की बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रोथ देखी, जिसकी वजह थी दुनिया भर में कम लागत वाले टीकों को डेवलप करने, मैन्युफैक्चर करने और सप्लाई करने की इसकी काबिलियत।5 जेनेरिक दवाओं के एक बड़े सप्लायर के तौर पर भारत अमेरिका जैसे विकसित बायोसिमिलर बाज़ार में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है।6
भारतीय कंपनियों का पिछले कई सालों से दुनिया भर के रेगुलेटेड बाज़ारों में दवा उत्पादों के एक्सपोर्ट का एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां उन्होंने कार्यकुशलता और लोकप्रियता दिखाई है। हालांकि, भारत में बनी दवाओं की क्वालिटी के बारे में हाल ही में गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं, खासकर ज़ाम्बिया में बच्चों की मौत जैसी घटनाओं के बाद जो भारत में बने कफ़ सिरप में पाए ज़हरीले पदार्थों से जुड़ी हैं।7 एक और मामले में, भारतीय दवा निर्माता इंटास की बनाई कैंसर की एक दवा पर लापरवाही और कमज़ोर नियम-कायदों का हवाला देते हुए अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था।8
हालांकि दुनिया भर में कम लागत की दवाएं सप्लाई कराने की भारत की क्षमता के बारे में सब जानते हैं, फिर भी भरोसा, विश्वसनीयता और लंबे समय तक कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए क्वालिटी को बनाए रखना ज़रूरी है।
भारत को बायोफार्मा वैल्यू चेन में आगे बढ़ने तथा ग्लोबल बायोफार्मास्युटिकल इनोवेशन हब बनने के लिए कई और चुनौतियों का समाधान करना होगा।9 इनमें से प्रमुख है उद्योग और शिक्षा जगत के बीच रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा बनाना और सेक्टर की तरक्की के लिए मददगार पॉलिसी मेकेनिज़्म तैयार करना।
रिसर्च के कारोबारी फायदे के लिए उद्योग-शिक्षा जगत का सहयोग
जब बुनियादी अनुसंधान और विकास (R&D) की बात आती है तो सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थान अक्सर अलग-अलग वजह और मकसद के साथ काम करते हैं, जिससे उनका काम एक-दूसरे से अलग-थलग रहता है।10 सरकारी लैब आमतौर पर हाई-क्वालिटी वाले एकेडमिक रिसर्च पेपर छापने के मकसद से लंबे वक्त के बुनियादी रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर कारोबारी फायदे की क्षमता वाले रिसर्च को प्राथमिकता देता है। एकेडमिक रिसर्च करने वालों के पास अक्सर इंडस्ट्री कनेक्शन की कमी होती है, जिससे अच्छे रिसर्च को बाज़ार के लिए तैयार प्रोडक्ट्स में बदलने में देरी हो सकती है।11
रोटावैक वैक्सीन एक बड़ी मिसाल है। हालांकि इस स्ट्रेन की खोज सबसे पहले 1985 और 1986 के बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), दिल्ली में की गई थी, लेकिन पहली कमर्शियल वैक्सीन 2016 में जाकर भारत बायोटेक ने बनाई थी।12
यह मामला दिखाता है कि भारत के बायोफार्मा सेक्टर में सरकारी-निजी सहयोग में कमी किस तरह से ज़रूरी हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स के कमर्शियल इस्तेमाल को धीमा कर सकती है, नहीं तो उनका इस्तेमाल लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए ज़्यादा तेज़ी से किया जा सकता था। शिक्षाविदों और निजी क्षेत्र के बीच जानकारी की साझेदारी को बढ़ाना दोनों पक्षों की अपनी-अपनी ताक़तों का फायदा उठाने और बायोफार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स की डिलीवरी बाज़ार में तेज़ी से करने के लिए अहम है।13 इस तरह के सहयोग, उन रोगाणुओं के खिलाफ़ वैक्सीन और दूसरे बायोफार्मा प्रोडक्ट्स के तेज़ विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, जो आने वाले वक्त में महामारी फैलाने की क्षमता रखते हैं।
एक विषय के लिए कई रेगुलेटर और नौकरशाही की रुकावटें
रोटावैक वैक्सीन को बाज़ार में लाने में देरी हुई क्योंकि अलग-अलग मंत्रालयों की एजेंसियों से कई तरह की मंज़ूरी लेने की ज़रूरत थी। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी (DBT) के तहत बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी एप्रूवल पोर्टल (BioRRAP) ने भारत में बायोलॉजिकल रिसर्च करने के लिए एप्लिकेशन प्रोसेस को आसान बना दिया है, लेकिन इस सिस्टम में अभी भी प्रोडक्ट के व्यापारिक इस्तेमाल की मंजूरी हासिल करने के लिए एक आसान प्रक्रिया की कमी है, जो एक बड़ी रुकावट है।14
भारत में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स अभी भी चार अलग-अलग मंत्रालयों के तहत आने वाले डिपार्टमेंट रेगुलेट करते हैं: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; रसायन और उर्वरक मंत्रालय; और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।15 इन मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी के साथ-साथ एप्लिकेशंस का काम आगे बढ़ने में आने वाली चुनौतियों की वजह से अक्सर कंपनियां नौकरशाही की देरी और उलझे हुए रेगुलेटरी प्रोसेस में फंस जाती हैं।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए, भारत सरकार ने सुधार लाने वाले कुछ कदम उठाए हैं। हाल ही में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपीय यूनियन के रेगुलेटरों से मंजूर अल्ज़ाइमर, वजन घटाने और कैंसर की दवाओं के लिए क्लीनिकल ट्रायल्स करने से छूट दी गई है।16 इस कदम से भारतीय बाज़ार में दवाएं उपलब्ध कराने में काफ़ी तेज़ी आई है और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हासिल कर चुकी भारतीय दवा निर्माताओं के लिए क्लीनिकल ट्रायल्स की लागत कम हो गई है, जिससे दवा की कीमत कम रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा कोरोनावायरस महामारी के दौरान, भारत में वैक्सीन और डायग्नॉस्टिक्स के व्यापारिक इस्तेमाल में तेज़ी लाने के लिए रेगुलेटरी मंजूरी की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया गया। एप्लिकेशन देने और उनके रिव्यू में तेज़ी लाने के लिए रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन को भी शुरू किया गया। इसलिए, ज़रूरी और नए बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ आपात स्थितियों में नहीं, बल्कि नियमित रूप से इन तरीकों को संस्थागत रूप देना महत्वपूर्ण है।
ऑनलाइन सबमिशन के लिए एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए ताकि एप्लिकेशन्स को ट्रैक किया जा सके और अलग-अलग रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स के बीच जानकारी साझा की जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि रिव्यू प्रोसेस को दोहराने के बजाय, एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय से मिली मंजूरी के बाद आगे की प्रक्रिया पर काम कर सकता है, जिससे रेगुलेटरी मंजूरी के लिए लगने वाला वक्त कम हो जाए। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का माहौल लागू करने से कंपनियों को रेगुलेटर की निगरानी के तहत अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की जांच करने के विकल्प मिल सकते हैं। इसके अलावा, रेगुलेटरी कर्मचारियों की ट्रेनिंग में निवेश करना भी ज़रूरी है ताकि कॉम्पलेक्स बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को संभालने और रिव्यू करने की उनकी काबिलियत बढ़ सके।
निष्कर्ष
भारत को बायोफार्मास्युटिकल इनोवेशन में आगे बढ़ने के लिए, रिसर्च को असरदार ढंग से बाज़ार में बिकने वाले प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए एकेडमिया-इंडस्ट्री के रिश्तों को बढ़ाना होगा। दवा की गुणवत्ता बनाए रखना “दुनिया की फार्मेसी” के रूप में अपनी ग्लोबल हैसियत को मज़बूत करने के लिए महत्वपूर्ण है और बायोफार्मा प्रोडक्ट्स को मंज़ूरी देने में तेज़ी लाने के लिए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। 2030 के अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, भारत को बायोफार्मास्युटिकल सेक्टर में अपनी ताक़त का फायदा उठाना चाहिए ताकि रिसोर्स-एफिशिएंट और इनोवेटिव बायोइकॉनमी का रास्ता तैयार हो सके।
भारत के स्पेस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना
परिचय
जून 2020 में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस (DoS) के तहत इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइज़ेशन (ISRO) ने भारत के स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने के लिए सुधार पेश किए।1 इन सुधारों के सपोर्ट में कई कदम उठाए गए हैं - इंडियन नेशनल स्पेस ऑथोराइज़ेशन एंड प्रोमोशन सेंटर (IN-SPACe) की स्थापना;2 लागू करने के दिशा-निर्देशों के साथ इंडियन स्पेस पॉलिसी 20233 जारी करना;4 और स्पेस सेक्टर के लिए सीधा विदेशी निवेश (FDI) नीति का उदारीकरण।5 इन सुधारों ने 630 बिलियन डॉलर के ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारतीय निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया और देश में 2023 तक 189 स्पेस स्टार्टअप शुरू कराए।6 इस वजह से ISRO को रणनीतिक कार्यक्रमों की तरफ धीरे-धीरे रुख करने की सुविधा भी मिली, साथ ही स्पेस कंपनियों सीधा व्यापारिक बाज़ार की ज़रूरत का ख्याल रख सकीं।
2023 में, IN-SPACe ने भारत के स्पेस सेक्टर के लिए दस सालों का एक विज़न और स्ट्रैटेजी जारी की, जिसमें भारत की स्पेस इकॉनमी को मौजूदा 8 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2033 तक 44 बिलियन डॉलर करने के उद्देश्य पर ज़ोर डाला गया।7 खास तौर पर, इस विज़न का मकसद 2033 तक भारत के स्पेस एक्सपोर्ट को 11 बिलियन डॉलर, लगभग 92,100 करोड़ रुपये तक बढ़ाना है - जो इसके बाज़ार लक्ष्य का एक-चौथाई है। इससे भारत के लिए अपने विज़न को साकार करने के लिए और साथ ही विदेश नीति साधन के रूप में भी स्पेस एक्सपोर्ट की अहमियत दिखती है।
2022-23 में भारत के स्पेस एक्सपोर्ट की वैल्यू 1,165.52 करोड़ रुपए (करीब 138 मिलियन डॉलर) से ज़्यादा थी, जिसमें लॉन्च सर्विसेज़, मिशन सपोर्ट सर्विसेज़, प्रोडक्ट्स और स्पेस सेगमेंट कम्युनिकेशंस शामिल थे।8 भारत के स्पेस एक्सपोर्ट को 2032-33 तक 11 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए हर साल 54.8 फीसदी की दर से बढ़ना चाहिए। इस लेख में, मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्पेस सेक्टर के लिए भारत के दीर्घकालिक लक्ष्यों के कामयाब होने की क्या संभावना है और साथ ही इन सवालों के जवाब ढूंढ़ने की कोशिश कर रहा हूं: क्या भारत अपने स्पेस एक्सपोर्ट टार्गेट को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? और ऐसा करने के लिए उसे अगले पांच से दस साल में क्या करने की ज़रूरत है?
| Financial Year | Exports (in crores Rs.) |
| 2019–20 | 287.53 |
| 2020–21 | 271.46 |
| 2021–22 | 188.40 |
| 2022–23 | 1165.52 < |
.png)
क्या भारत 2033 तक स्पेस एक्सपोर्ट में 11 बिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के रास्ते पर है?
विशेषज्ञों का मानना है कि दस साल के विज़न में एक्सपोर्ट के अनुमान महत्वाकांक्षी हैं और मौजूदा स्थिति में इन्हें हासिल करना मुश्किल लगता है।9 हालांकि, उनका यह भी मानना है कि ऐसी महत्वाकांक्षा भारत के स्पेस सेक्टर को 11 बिलियन डॉलर के लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए प्रेरित कर सकती है।10
इस लक्ष्य के करीब पहुंचने के रास्ते की शुरुआती चिंताओं में से एक यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत के स्पेस एक्सपोर्ट में गिरावट आई है [ऊपर के आंकड़े देखें], सिर्फ़ 2022-23 में इसरो के आठ विदेशी कमर्शियल पेलोड लॉन्च करने से होने वाली बढ़ोतरी को छोड़कर।11 सितंबर 2024 तक, इसरो ने एक भी विदेशी कमर्शियल पेलोड लॉन्च नहीं किया था।12 इसके अलावा, 2023-24 में, सर्विसेज़ को छोड़ दें तो सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल एक्सपोर्ट $1.79 मिलियन था, जो 2022-23 के मुकाबले 93 फीसदी कम है। 2023-24 के लॉन्च मेनिफेस्ट के मुताबिक, इसरो ने 2024 के अंत में केवल एक विदेशी पेलोड लॉन्च शेड्यूल किया था - यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) का प्रोबा-VI।13 इसके अलावा, 2023-24 के लिए भारत के कुल स्पेस एक्सपोर्ट का अनुमान अभी देखा जाना बाकी है।
इस अवधि में, अमेरिका और जापान जैसे देशों के स्पेस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है।14 स्पेस में उड़ान भरने वाले दूसरे देशों के साथ मुकाबला करने और अपने स्पेस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, भारत को कुछ चुनौतियों के बारे में सोचना होगा।
लॉन्च मार्केट में दूसरों से मुकाबले की काबिलियत को बढ़ाना
इसरो के चेयरपर्सन एस. सोमनाथ के मुताबिक, सैटेलाइट एप्लिकेशंस के लिए आंतरिक (घरेलू) मांग घटने की वजह से भारत की लॉन्च सर्विसेज़ की मांग में गिरावट आई है।15 घरेलू मांग की यह कमी लॉन्च एक्सपोर्ट पर असर डालती है क्योंकि स्पेस लॉन्च आम तौर पर राइड-शेयर बेसिस पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि इसरो को तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि भारत के भीतर और बाहर से आने वाले ऑर्डर उसकी लॉन्च व्हीकल कैपेसिटी को पूरा कर दें, और इस वजह से व्हीकल लॉन्च में देरी हो सकती है। यह दिक्कत इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के बनने के बाद से ही रही है, जिसने सप्लाई पर आधारित मॉडल को बदलकर डिमांड पर आधारित मॉडल अपनाया है।16
लेकिन लॉन्च एक्सपोर्ट डिमांड को बढ़ाने के लिए घरेलू मांग से आगे जाकर, भारत को ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में खुद को मुकाबले में बनाए रखने की ज़रूरत है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ऑन-डिमांड सर्विस और बड़े सैटेलाइट लॉन्च करने की सर्विस देना। जहां स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) के सफल परीक्षण दिखाते हैं कि छोटे, ऑन-डिमांड लॉन्च की दिशा में तरक्की हो रही है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने बताया है कि आगे जाकर स्पेस इकॉनमी की ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा सैटेलाइट कम्युनिकेशन से आएगा - ऐसी सर्विसेज़ जिनके लिए भारी लॉन्च व्हीकल्स की ज़रूरत होगी।17
हालांकि इसरो ने पहले एक साथ कई सैटेलाइट कामयाबी के साथ लॉन्च किए हैं, लेकिन फिलहाल इसके पास स्पेस-एक्स के फाल्कन हेवी या फाल्कन 9 जैसा भारी-भरकम लॉन्च व्हीकल नहीं है, जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेश सर्विस के लिए एक से ज़्यादा सैटेलाइटों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है।18 वर्तमान में, इसरो का LVM-3 केवल 4 टन वज़न को जियोसिन्क्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में और 10 टन वज़न को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में ले जा सकता है, जबकि फाल्कन 9, 8 टन वज़न को GTO में और 22 टन वज़न को LEO में ले जा सकता है। वहीं स्पेस-एक्स फाल्कन हेवी 27 टन वज़न को GTO में और 64 टन वजन को LEO में ले जा सकता है।19 इसके अलावा, फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी 2,500 डॉलर और 1,500 डॉलर प्रति किलोग्राम के सस्ते लॉन्च ऑप्शंस देते हैं, जबकि इसरो LVM-3 की पेशकश है 10,500 डॉलर प्रति किलोग्राम।20
इस तरह, लॉन्च में देरी, लॉन्च सर्विस में दूसरों से कंपिटिशन में पिछड़ना और ऊंची लागत अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को दूसरे लॉन्च सर्विस प्रोवाइडरों की तरफ मोड़ सकती है। अगर इसे अनदेखा किया गया तो भविष्य में लॉन्च एक्सपोर्ट के मौके हासिल करने में भारत को नुकसान पहुंच सकता है।
सैटेलाइट एप्लिकेशंस के लिए लगातार घरेलू मांग तैयार करना
अर्थ ऑब्ज़र्वेशन, नेविगेशन और कम्युनिकेशन जैसे सैटेलाइट एप्लिकेशंस के लिए लगातार घरेलू मांग बनाए रखना लॉन्च सर्विसेज़, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस डोमेन अवेयरनेस, और इन-ऑर्बिट सर्विसिंग की मांग बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। लगातार घरेलू मांग बनाए रखने की काबिलियत में कमी की वजह से भारतीय स्पेस कंपनियां बाज़ार से बाहर हो सकती हैं, जिससे भारत के स्पेस एक्सपोर्ट के मौके घट सकते हैं।21 घरेलू बाज़ार को मज़बूत करने से निवेश आएगा, क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलेगी और नए बिज़नेस हासिल करने में तेज़ी आएगी। घरेलू ग्राहकों की मांग पूरी करने से विदेशी ग्राहक और ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं।
भारत में सैटेलाइट एप्लिकेशंस की कम घरेलू मांग के बारे में इसरो चेयरपर्सन की चिंता को भारत में स्पेस एप्लिकेशंस के बारे में जागरूकता की कमी और मांग को बढ़ाने के लिए एक मज़बूत इकोसिस्टम की ज़रूरत से जोड़कर देखा जा सकता है, जिसमें सरकार एक प्रमुख ग्राहक है।22
बेहतर सैटेलाइट सर्विसेज़ की मांग सरकार के भीतर से भी बढ़ाई जा सकती है। जैसे, 2024 में वायनाड में ज़मीन खिसकने के हादसे के बाद, भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने सैटेलाइट सर्विसेज़ की सीमाओं की तरफ ध्यान दिलाया, जिस वजह से बादल फटने और ज़मीन खिसकने का पता नहीं लगाया जा सका।23 बेहतर सैटेलाइट सर्विसेज़ से आपदा के दौरान कई मौतों को रोका जा सकता था। इसी तरह, ज़्यादा मंत्रालय, सिविक बॉडीज़ और बिज़नेस अपनी दिक्क़तों को हल करने के लिए सैटेलाइट सर्विसेज़ का फायदा उठाने के मौकों की खोज और पहचान कर सकते हैं।
हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं?
सबसे पहले, लॉन्च एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, भारत को लागत और इंतज़ार के समय को घटाना चाहिए।24 SSLV की तकनीक का व्यापारिक इस्तेमाल करते हुए इसे प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करके और कुलसेकरपट्टिनम में दूसरे लॉन्चपैड को चालू करके यह किया जा सकता है।25 इससे कस्टम ऑन-डिमांड लॉन्च और लॉन्च एक्सपोर्ट के मौके बढ़ाने में मदद मिल सकती है। भारत का भारी और दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्चर का विकास इसे लॉन्च बाज़ार में कंपिटिटिव बना सकता है और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है।26 इसके अलावा, भारत के स्पेस लॉन्च स्टार्टअप की तरक्की को देखते हुए, अगर बाज़ार के लिए उन्हें तैयार करने के काम में तेज़ी लाए जाए तो लॉन्च ऑप्शंस भी बढ़ सकते हैं, देरी कम हो सकती है और भारत का लॉन्च एक्सपोर्ट बढ़ सकता है।27
दूसरे कदम के तौर पर, सरकारी खरीद कार्यक्रम कई भारतीय स्पेस कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट केपेबिलिटी तैयार करने और उन्हें बढ़ाने के लिए लगातार घरेलू मांग पैदा कर सकते हैं।28 जिस तरह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के ज़रिए लॉन्च व्हीकल्स और अर्थ ऑब्ज़र्वेशन (EO) सैटेलाइट की खरीद शुरू की है, उसी तरह सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए कार्यक्रमों का होना फायदेमंद हो सकता है।29 जल शक्ति मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जैसे दूसरे विभागों को भी रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भारतीय कंपनियों से सीधे अर्थ ऑब्ज़र्वेशन डेटा और दूसरे सैटेलाइट एप्लिकेशंस के लिए खरीद कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए हासिल ओपन स्पेस डेटा और टूल्स भारतीय कंपनियों को वैल्यू की पहचान करने और सैटेलाइट एप्लिकेशंस तैयार करने में मदद कर सकते हैं, जिससे ऐसे एप्लिकेशंस के लिए जागरूकता, सप्लाई और अंत में मांग को बढ़ावा मिलेगा।30
तीसरे कदम के तौर पर भारत को इंडो-पैसिफिक, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में अपनी भागीदारी को बढ़ाना जारी रखना चाहिए। वैसे तो अमेरिका के साथ इनीशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET) और फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी ने भारत के स्पेस प्राइवेट सेक्टर के लिए मौके बनाए हैं, लेकिन विकसित अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाओं से आगे देखना भी ज़रूरी होगा।31 2019 से, भारत की लॉन्च सर्विसेज़ यूरोप, जापान, सिंगापुर और अमेरिका तक सीमित रही हैं। हाल के महत्वपूर्ण कदमों से बाकी इलाकों में भी भागीदारी की संभावना का संकेत मिलता है। जून 2024 में, भारत और केन्या ने अंतरिक्ष सहयोग स्थापित किया और अगस्त 2024 में, NSIL ने नेपाली सैटेलाइट के लॉन्च में मदद के लिए एक करार पर दस्तखत किए।32 इन इलाकों में कारोबारी पहुंच बढ़ाने से भारत को उनकी बाज़ार क्षमता को देखते हुए अपने स्पेस एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ाने में मदद मिलेगी।33 फिलहाल इसरो की सिर्फ़ मॉस्को, पेरिस और वॉशिंगटन डीसी में तकनीकी सहयोग बढ़ाने वाली यूनिट हैं जो इन देशों में द्विपक्षीय सहयोग का रास्ता तैयार करती हैं।34 अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भारतीय मिशनों में ऐसी ही यूनिट बनाना और बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए खास अफसर नियुक्त करना भारत को एक्सपोर्ट के मौके पहचानने और उनका फायदा उठाने में मदद कर सकता है।
*लेखक कार्नेगी इंडिया के इंटर्न्स जिया मुखर्जी, अर्नव भसीन और मो एरियोशी को उनकी कीमती मदद के लिए शुक्रिया करना चाहते हैं।
डिजिटल ट्रांज़िशन में भारत की साइबर चुनौती
भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को हर कोई एक शानदार कामयाबी मानता है।1 भारत के डिजिटल फुटप्रिंट की बुनियाद और पैमाना चौंकाने वाला है - 93.62 करोड़ इंटरनेट ग्राहक, हर महीने 14 अरब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लेन-देन, जो रोज़ाना 50 करोड़ होने जा रहे हैं, और 1.4 अरब आधार।2 आज करीब-करीब सभी सरकारी सर्विसेज़ डिजिटल हो गई हैं, जिनमें पहचान, बैंकिंग प्रोसेस, पेमेंट गेटवे, सोशल सेक्टर में दखल, डिजिटल सर्विसेज़, पर्यटन, यात्रा, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं - इन सभी डोमेन में डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनी पैठ बना चुकी हैं।
6G टेक्नोलॉजी दस्तक दे रही है, और रोज़ की ज़िंदगी से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तेज़ी से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा बन रही हैं। यानी हमारे काम आने वाली चीज़ें कंप्यूटर से जुड़ी हैं, और कंप्यूटर की तरह काम करती हैं - कार, रेफ्रिजरेटर, घड़ियां, टेलीविज़न सेट और मोबाइल फ़ोन, यहां तक कि इंसुलिन पंप और डिफिब्रिलेटर जैसे मेडिकल इक्विपमेंट भी।3 इससे इन चीज़ों पर डिजिटल तरीके से निगरानी रखी जा सकती है या कंट्रोल किया जा सकता है।
जैसे-जैसे भारत में डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे उनकी कमज़ोरियों पर हमला करने की रफ्तार भी बढ़ रही है।4 इंसान अब एक ऐसे साइबरस्पेस में रहते हैं, जहां उन्होंने "ऑफ़लाइन" होने का विकल्प छोड़ दिया लगता है - बदकिस्मती से इसका मतलब यह भी है कि सब कुछ हैक किया जा सकता है।
इस साइबरस्पेस को सुरक्षित किया जाना चाहिए, न सिर्फ़ इसलिए कि यही वो अहम इलाका है जहां दुश्मनों से लड़ा जाता है, बल्कि इसलिए भी कि यह इंसानी ज़िंदगी से गहरे तक जुड़ा हुआ है। यह साइबरस्पेस आर्थिक हलचल, बिज़नेस, लोकतांत्रिक मताधिकार के प्रयोग, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, विवाद और यहां तक कि युद्ध का भी केंद्र बन रहा है।
आज की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और साइबर हाइजीन और सिक्योरिटी से कहीं आगे जाती हैं। इनसे निपटने के लिए एक मज़बूत साइबर फाउंडेशन बनाए रखना होगा जो साइबर हमलों के ख़तरे के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता के लिए ज़रूरी हैं। साइबर फाउंडेशन यानी सुरक्षित नेटवर्क, मज़बूत प्रोटोकॉल, जोखिम कम करने की रणनीति, स्किल्ड वर्कफ़ोर्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। भारत में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट के तहत नेशनल साइबरसिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर (NCSC) को साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर अलग-अलग एजेंसियों और विभागों के साथ तालमेल करने की जिम्मेदारी मिली है।5 2018 में बनाई गई इंटेग्रेटेड ट्राई-सर्विस एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी (DCA), भारत की साइबर प्रतिरोधक क्षमता पक्की करने के लिए ज्वॉइंट साइबर ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है।6 मोटे तौर पर, एक मज़बूत साइबर बुनियाद बनाने का काम NCSC का होना चाहिए, और साइबर प्रतिरोधक क्षमता DCA का। दोनों डोमेन गहराई से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे पर निर्भर भी हैं; एक की कमज़ोरी दूसरे को भी कमज़ोर करेगी। इसलिए NCSC और DCA को एक साथ जोड़ा जाना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल, इस तरह के एकीकरण पर अभी भी कदम उठाने की ज़रूरत है।
साइबर फाउंडेशन
एक मज़बूत साइबर फाउंडेशन का मतलब है साइबरस्पेस को सुरक्षित, लचीला, सुलभ और निष्पक्ष बनाए रखना। यह समृद्धि और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, और भरोसे के साथ राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ज़रूरी है - एक ऐसे इलेक्ट्रिकल ग्रिड को बनाना जो बिलकुल सटीक ढंग से दूर तक फैले इलाके में रिन्युएबल एनर्जी पहुंचा सके; हाई बैंडविड्थ वाला तेज़ संचार जो सहयोग, व्यापार और सांस्कृतिक लेन-देन को मुमकिन करता हो; एक फ्री, ओपन और सुरक्षित इंटरनेट जो हमारे लोकतंत्र के लिए सार्थक हो।
यूक्रेन में युद्ध के शुरुआती दिनों में, रूस ने यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम और अन्य ग्रिडों पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले किए, जो इतने गंभीर थे कि यूक्रेन की सरकार को अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट की मदद से कुछ ही दिनों में क्लाउड पर माइग्रेट करने के लिए मजबूर होना पड़ा।7
साइबर मोबिलाइज़ेशन और क्लाउड पर माइग्रेशन के लिए भारत की क्या योजनाएं हैं (अगर कोई हैं)?
भारत का मुख्य और चाहत भरा उद्देश्य शायद एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना होगा जो स्वाभाविक रूप से सुरक्षित और लचीला यानी किसी तरह के झटके से तुरंत भरपाई करने वाला हो। ये न केवल बहुत बड़ी चाहत हैं, बल्कि बड़ी चुनौतियां भी हैं।
सुरक्षित का मतलब है कि हमले की स्थिति में बचाव करने वाला मज़बूत पोज़िशन में हो, और इसके लिए ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना होगा जिसमें सुरक्षा उपायों या डिजिटल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को योजना बनाकर, सावधानी से सोच-विचार करने के बाद शुरू से ही शामिल किया जाए, न कि सिस्टम के बन जाने के बाद उन्हें जोड़ा जाए।
लचीलेपन का मतलब है यह पक्का करना कि जब साइबर डिफेंस नाकाम हो जाए, जो कि कभी-कभी हो सकता है, तो नतीजे विनाशकारी नहीं हों। रिकवरी आसान और तेज़ होनी चाहिए, और साइबर घटनाओं का असर ना तो सिस्टम पर आए और ना ही बहुत दूर तक फैले।
साइबर प्रतिरोधक क्षमता
भारत के पास अच्छे संसाधन वाली एक ऐसी सेना है जो ज़मीन, हवा और समुद्री सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसी तरह DCA को लगातार बढ़ते भारतीय साइबरस्पेस को सुरक्षित करने के लिए हमलों को रोकने का काम सौंपा गया है।8 युद्ध अब साइबरस्पेस तक फैल गया है, और शायद अब वक्त आ गया है कि DCA को पूरी तरह एक लड़ाकू कमांड में अपग्रेड किया जाए, रैंक और स्टेटस अपग्रेड के ज़रिए नहीं बल्कि रियल-टाइम ऑपरेशनल कैपेसिटी विकसित करके। आधुनिक सेनाओं में साइबर कमांड ने दुश्मन के शहरों को ठप्प करने के लिए साइबर एक्सप्लॉइट (कोड या प्रोग्राम का हिस्सा जो गलत तरीके से सॉफ़्टवेयर या हार्डवेयर में कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाता है) विकसित किए हैं जो एनर्जी ग्रिड, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डेटाबेस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लॉजिस्टिक्स ग्रिड और शहर के कामकाज के लिए ज़रूरी कई और डिजिटल सिस्टम को निशाना बनाते हैं। जैसे, मई 2017 में नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) को निशाना बनाने वाले रैनसमवेयर WannaCry के पीछे का मालवेयर यू.एस. नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने बनाया था, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे गलत इरादे से चुराया गया था। AI-इनेबल्ड साइबर एक्सप्लॉइट भी विकसित किए जा रहे हैं और उन्हें रोकना करीब-करीब नामुमकिन है।9
क्या हो सकता है: रोडमैप
ऊपर की चर्चा के संदर्भ में, नीचे बताई गई दस बातें शायद आगे का रास्ता दिखा सकती हैं-
1. NCSC और DCA मिलकर भारत के लिए 20 पन्नों की एक साइबर रणनीति तैयार कर सकते हैं, जिसमें साइबर फाउंडेशन बनाने और साइबर प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए योजनाओं की साफ़ रूपरेखा हो।
2. इसके बाद NCSC को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को सुरक्षित और लचीला बनाने के लिए पूरा ब्यौरा तैयार करना चाहिए। पावर ग्रिड, पानी की सप्लाई के सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जैसे अहम बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने की ज़रूरत होगी। डिजिटल लिगेसी सिस्टम को मौजूदा साइबर स्टैंडर्ड्स के साथ अपजेट करना भी ज़रूरी है।
3. DCA को साइबरस्पेस के लिए योजनाएं बनानी चाहिए और आक्रामक क्षमताएं विकसित करनी चाहिए, जिनमें साइबर एक्सप्लॉइट विकसित करना और साइबर प्रतिरोधक क्षमता के लिए भरोसेमंद ढांचे बनाना शामिल है। इस बात को समझा जाना ज़रूरी है कि असरदार साइबर प्रतिरोधक क्षमता के लिए आक्रामक साइबर क्षमताओं का कोई और विकल्प नहीं है। हालांकि, इस तरह के ढांचे का ब्यौरा साफ़ तौर पर गोपनीय रहेगा।
4. फायरवॉल बनाने और सुरक्षित क्लाउड तक ट्रांज़िशन के लिए पूरे ब्यौरे के साथ एक योजना भी विकसित करने की ज़रूरत होगी।
5. देश के डिजिटल इकोसिस्टम को सुरक्षित और लचीला बनाने का काम, इसके पैमाने पर विशेषज्ञों की ज़रूरत को देखते हुए, सिर्फ़ सरकार के कंधों पर नहीं डाला जा सकता। एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल विकसित करना होगा, जिसमें साइबर स्टार्टअप को ज़रूरी प्रोत्साहन और आमदनी वाले मॉडल के साथ इस काम में जोड़ा जाना चाहिए।
6. निगरानी रखने, सांस्कृतिक असर और कूटनीति को साइबरस्पेस में शामिल किया जा रहा है। पश्चिमी लोगों के बर्ताव को बदलने के लिए चीन की तरफ से टिकटॉक का इस्तेमाल एक एल्गोरिदमिक उपकरण की तरह किया जाना इसका उदाहरण है।10 इस बारे में पूरे ब्यौरे के साथ एक्शन प्लान डेवलप किया जा सकता है।
7. दुनिया डिजिटल डिवाइड (उन लोगों के बीच का अंतर जिनके पास इंटरनेट और तकनीक तक पहुंच है और जिनके पास नहीं है) की तरफ़ तेज़ी से बढ़ सकती है, और शायद इंटरनेट अलग-अलग कई नेटवर्कों में बंट सकता है।11 इस वजह से ग्लोबल साइबर गवर्नेंस के ढांचों पर दबाव दिखता है। बेहतर होगा कि भारत की भावी साइबर रणनीति में आने वाली खामियों, इंटरनेट की भौगोलिक स्थिति, समुद्र के नीचे केबल की सुरक्षा की जांच जैसे मुद्दे शामिल हों और साथ ही एक माकूल प्रतिक्रिया के बारे में भी सोचा जाए।
8. साइबरस्पेस में चुनौतियों का हल करने के लिए भारत को जिस तरह के टैलेंट और स्किल की ज़रूरत होगी, उनका अनुमान लगाना और उसके मुताबिक मानव पूंजी विकसित करने की योजना बनाना भी फायदेमंद होगा।
9. एक के बाद एक लगातार आ रही टेक्नोलॉजीज़ की वजह से साइबर लैंडस्केप तेज़ी से विकसित हो रहा है - खास तौर पर AI, अंतरिक्ष, चिप्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी। भविष्य के बारे में सोचकर बनाए जाने वाले भारतीय साइबर प्रोजेक्ट को इस तरह की तकनीक के फायदों को ध्यान में रखना चाहिए।
10. यह एक ग़लतफ़हमी है कि साइबर डोमेन का मतलब सिर्फ तकनीक है, या सिर्फ़ कोडिंग और एल्गोरिदम है। भले ही तकनीक महत्वपूर्ण है, साइबर डोमेन में उतनी ही अहमियत भू-राजनीतिक ढांचे की है। इन बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई साइबर रणनीति भारत को भविष्य में आगे रहने में मदद करेगी, वरना यह दूसरों की बराबरी पर आने की कोशिश भर करता रहेगा।