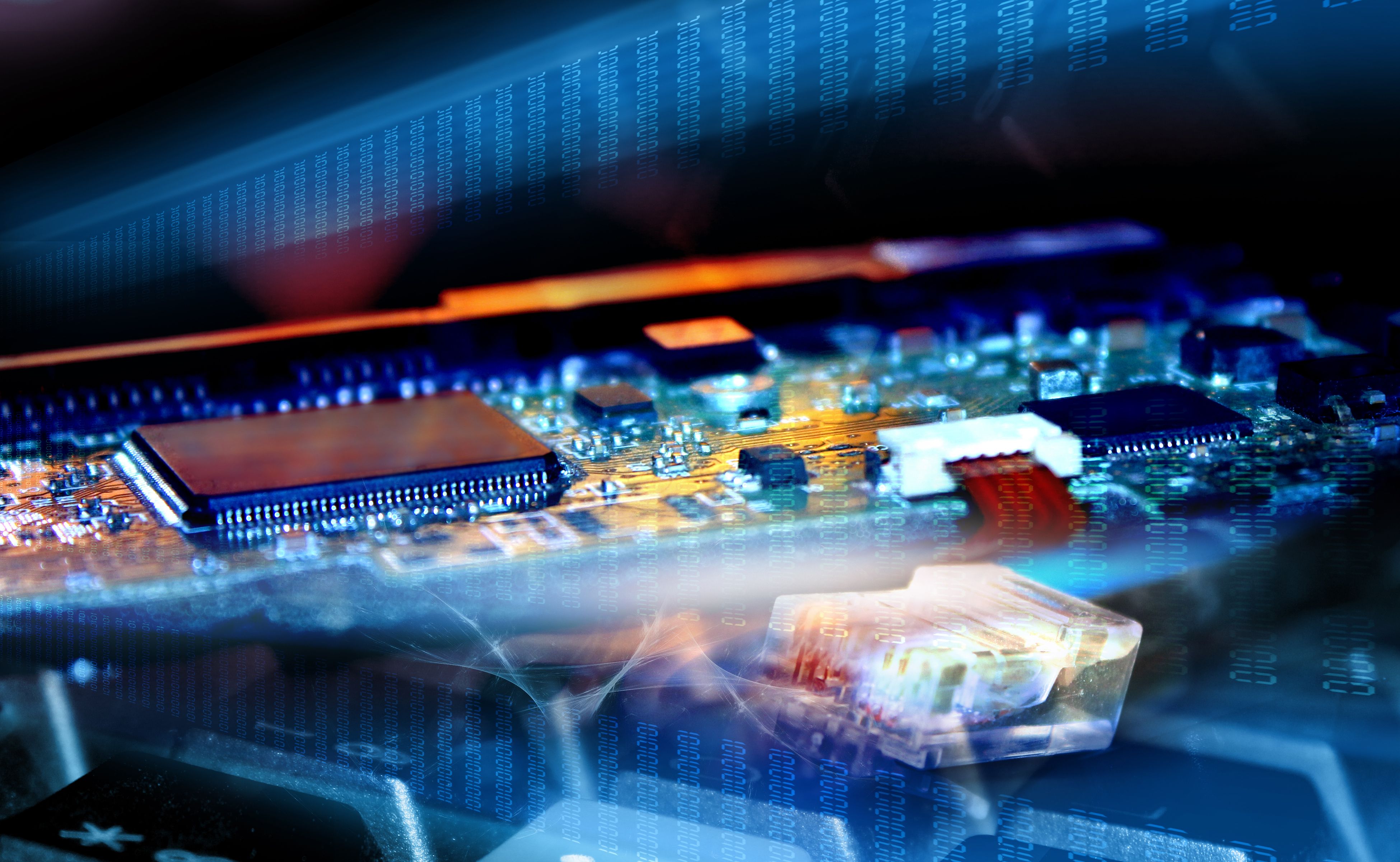भारत ने आज़ादी के बाद से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की कई बार कोशिश की, लेकिन इन कोशिशों के नतीजे मिले-जुले रहे, और कई बार अच्छे इरादों से की गई शुरुआत आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि, दिसंबर 2021 में, भारत ने एक मज़बूत सेमीकंडक्टर नेटवर्क विकसित करने की कोशिश दोबारा शुरू की। इस बार, यह पहल अच्छी तरह आगे बढ़ रही है और कोई बड़ी रुकावट नहीं आई है।
इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की स्थापना केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत एक मुख्य एजेंसी के तौर पर की गई ताकि देश में निवेशों की जांच हो और सेमीकंडक्टर स्कीमों को लागू किया जा सके। पिछले चार साल से भी कम समय में, इसने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लगभग 10 अरब डॉलर के बड़े फैब निवेश से लेकर माइक्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ से असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) प्लांट लगाने के लिए 2.75 अरब डॉलर से ज़्यादा का निवेश शामिल है। दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं असम में एक OSAT (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर एसेंबली एंड टेस्ट) प्लांट; गुजरात के साणंद में दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स; और उत्तर प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर प्लांट।
12 अगस्त, 2025 को चार नए प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गई। इनमें ओडिशा में अलग से पैकेजिंग प्लांट, आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और पंजाब के मोहाली में पहले से मौजूद एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का विस्तार शामिल है। हालांकि अंदाज़ है कि लगभग 10 अरब डॉलर के शुरुआती फंड में से कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन सटीक आंकड़ा सामने नहीं आया है।
ISM के लॉन्च होने के चार साल बाद अब यह साफ़ दिख रहा है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम आगे बढ़ने की क्षमता दिखा रहा है। यह लेख भारत की अब तक की सेमीकंडक्टर यात्रा की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालता है।
भारत और चीन के नज़रिये में बड़ा फर्क
भारत की तरह चीन भी अपना मज़बूत घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग खड़ा करना चाहता है। चीन के मकसद में तकनीकी आत्मनिर्भरता की बड़ी रणनीति, अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल से मिली चुनौती, और अमेरिकी हिस्सों पर निर्भरता कम करने जैसी बातें शामिल मानी जाती हैं।लेकिन चीन का सेमीकंडक्टर बाज़ार "अंदर की ओर देखने वाला" ज़्यादा माना जाता है, जो शायद बाज़ार में मौजूद दुनिया की सबसे अच्छी सेमीकंडक्टर कंपनियों, जिनमें से ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप में हैं, के साथ मिलकर काम करने के बजाय पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की चाहत से प्रेरित है।
दूसरी तरफ, भारत ने ऐसा नज़रिया अपनाया है जिसमें बड़ी एंकर कंपनियों, अक्सर अमेरिकी कंपनियों को भारत लाने की कोशिश की जाती है। इसका फायदा यह होता है कि सिर्फ एंकर कंपनी ही नहीं, बल्कि उसकी सप्लाई चेन और बाकी सहयोगी कंपनियां भी भारत में आ जाती हैं। भारत ने यह तरीका दूसरे सेक्टरों में भी अपनाया है—जैसे ऐपल को अपनी असेंबली कामकाज और सप्लायर इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा भारत लाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया; इसी तरह की कोशिशें टेस्ला और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) सेक्टर में भी की गई हैं।
इसके साथ ही, भारत अपनी घरेलू कंपनियों को भी प्रोत्साहित कर रहा है कि वे नए विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर हब और क्लस्टर्स में निवेश करें और छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और OSAT प्लांट्स लगाने पर ध्यान दें।
पूंजी के मामले में, चीन ने अपनी सेमीकंडक्टर यात्रा में भारत के मुकाबले कहीं ज़्यादा फंड लगाया है, हालांकि इतना पैसा लगाने के बावजूद इसके नतीजे मिले-जुले रहे हैं। हालांकि, चीन अब भी यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है कि वह उन तकनीकों का अपना संस्करण विकसित कर सके, जो आज सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में सबसे बड़ी रुकावटें मानी जाती हैं।
भारत के प्रयास धीरे-धीरे रंग ला रहे हैं
सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को अपने देश में लाना (onshoring) एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें कई कंपनियां जुड़ी होती हैं और साथ ही अलग-अलग देशों की आकर्षक नीतियों से मुकाबला करना पड़ता है। इस संदर्भ में, वैश्विक व्यापार में हो रहे बड़े बदलावों ने भारत की मदद की है। मिसाल के लिए, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका की व्यापार नीतियों से सप्लाई चेन ऑनशोरिंग के मामले में भारत दुनिया की शीर्ष छह अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा। भारत से आगे जो देश रहे, उनमें से ज़्यादातर पहले से ही ग्लोबल वैल्यू चेन में अच्छी तरह जुड़े हुए थे। जैसे कि वियतनाम, जिसे अमेरिका की व्यापार नीतियों का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, वह पहले से ही चीन और दूसरे देशों के साथ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) जैसे समझौतों का हिस्सा था। जहां अमेरिका-चीन के बीच व्यापार बढ़ने की रफ़्तार बाकी देशों के साथ इन दोनों देशों के व्यापार बढ़ने के मुकाबले 30% धीमी पड़ी, वियतनाम जैसे देशों से अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ा। यह शायद इस बात का संकेत है कि सप्लाई चेन पूरी तरह से वियतनाम में शिफ्ट नहीं हुई, बल्कि टैरिफ़ की वजह से केवल लंबी और जटिल हो गई।
यह तथ्य भारत की प्रगति को और भी उल्लेखनीय बनाता है, क्योंकि भारत RCEP या कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफ़िक पार्टनरशिप (CPTPP) जैसे किसी बड़े बहुपक्षीय व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं है। मूडीज़ की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों की तरह, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए नए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने में अच्छा प्रदर्शन किया है। अप्रैल 2025 में घोषित की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम में निवेश बढ़ेगा, जिसके असर से देश में अपस्ट्रीम सेमीकंडक्टर निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।
क्रमबद्ध केंद्र-राज्य प्रक्रिया का लागू होना
कई भारतीय राज्यों ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी की हैं, और उनमें से गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और असम की नीतियों की समीक्षा हुई है। ये सभी राज्य केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स को "पात्र" मानते हैं जिन्हें ISM (इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन) ने मंज़ूरी दी हो। एक बार मंज़ूरी मिलने के बाद, राज्य आपस में मुकाबला करके केंद्र सरकार से मिलने वाले प्रोत्साहन के अतिरिक्त अपनी ओर से भी फायदे देने की कोशिश करते हैं। (इसका एक अपवाद ओडिशा की सेमीकंडक्टर स्कीम है, जो आईएसएम से मंज़ूर नहीं की गई परियोजनाओं को भी प्रोत्साहन देती है।)
यह संरचना यूरोपीय यूनियन के समान है, जहां चिप्स फॉर यूरोप इनीशिएटिव का मकसद “संघ और राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे फंडिंग कार्यक्रमों के बीच बेहतर तालमेल और जुड़ाव बनाना” है। यह अमेरिका के नज़रिये के समान भी है, हालांकि वहां उसका क्रम भारत के उलट है। अमेरिका के चिप्स एंड साइंस एक्ट के तहत किसी भी आवेदक के लिए ज़रूरी है कि "सुविधा के निर्माण, विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए उस प्रोजेक्ट की जगह वाले राज्य या स्थानीय प्रशासन से प्रोत्साहन" पहले सुनिश्चित किया जाए।
भारतीय राज्य प्रोत्साहन देने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं
यह बात बिल्कुल साफ़ है कि राज्यों से मिलने वाले प्रोत्साहन केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाले प्रोत्साहनों से अलग होते हैं, और उस इंडस्ट्री में काम कर रही कंपनियां अपनी पसंद के किसी भी राज्य में कामकाज शुरू कर सकती हैं। इसका अच्छा उदाहरण है टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (TSAT), जिसने असम में एक OSAT प्लांट लगाने का फ़ैसला लिया। TSAT ने असम में निवेश इस तथ्य के बावजूद किया कि ज़्यादातर लोगों का मानना था कि असम (उस समय तक) न तो सेमीकंडक्टर निवेश का पारंपरिक केंद्र है, और न ही उसकी वित्तीय प्रोत्साहन योजना सबसे अच्छी है।
गुजरात अग्रणी बनकर सामने आया
कई लोगों का मानना है कि उद्योग जगत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश के लिए गुजरात को इसलिए चुना है क्योंकि यहां फ़ैसले सर्वोच्च स्तर पर लिए जाते हैं और फिर उन्हें लागू किया जाता है। हालांकि, गुजरात नीचे बताई गई वजहों से निवेश आकर्षित करने में कामयाब माना जा सकता है:
- एक डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी: गुजरात पहला राज्य था जिसने एक डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की। कर्नाटक जैसे दूसरे राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से निवेश आकर्षित करने के लिए इंसेटिव स्कीम और नीतियां पहले से मौजूद थीं। हालांकि, उन राज्यों की पहले से मौजूद नीतियों का फोकस विशेष तौर पर सेमीकंडक्टर पर नहीं, बल्कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर था।
- क्लस्टर का फायदा: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्लस्टर में सबसे अच्छा काम करता है, जहां वैल्यू चेन के मुख्य खिलाड़ी एक-दूसरे के नज़दीक होते हैं। करीब 900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (धोलेरा SIR) को एक बड़ी डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर पेश किया गया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश भी इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशिष्ट क्लस्टर के साथ मुकाबले में हैं। हालांकि, ये ब्राउनफील्ड क्लस्टर हैं, जिनका फोकस सिर्फ़ सेमीकंडक्टर पर नहीं हैं और ये धोलेरा SIR के जैसे बड़े स्तर के भी नहीं हैं। गुजरात के दो प्रमुख बंदरगाहों से नज़दीकी जैसी वजहों से भी धोलेरा SIR को भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर निवेश स्थलों पर बढ़त दिखती है।
- माइक्रोन का निवेश बना तेज़ी लाने की वजह: 2023 मेंमाइक्रोन टेक्नोलॉजी का भारत के (और खासकर गुजरात के) सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में निवेश, भारत की केंद्र और गुजरात सरकार की भारी सब्सिडी के बावजूद, एक बड़ा बदलाव लेकर आया। माइक्रोन अपने साथ सप्लायर्स, सब-सप्लायर्स और दूसरी कंपनियों का एक पूरा इकोसिस्टम भारत लेकर आई। माइक्रोन का निवेश इस बात का सबूत भी था कि भारत का सेमीकंडक्टर माहौल बिज़नेस के लिए तैयार है
- प्रोजेक्ट को असरदार ढंग से लागू करना: कभी-कभी केवल इंसेंटिव की बात नहीं होती, बल्कि कदम उठाने में पहल करने का फायदा होता है, जो तेज़ी से प्रोजेक्ट का काम खत्म करने से मिलता है। मिसाल के लिए, उत्तर प्रदेश भी रोजगार पैदा करने और औद्योगिकीकरण के मामले में एक महत्वपूर्ण राज्य है। भारत के राजनीतिक परिदृश्य में हर चुनाव चक्र में भी इसकी एक बड़ी भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन देता है। दरअसल, यह इकलौता राज्य है जो "भारत सरकार से मंज़ूर प्रोजेक्ट की कुल लागत पर 100 प्रतिशत तक" प्रोत्साहन की पेशकश करता है। फिर भी, उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है।
इसकी तुलना गुजरात की सेमीकंडक्टर पॉलिसी में मिलने वाली “अतिरिक्त पूंजी सहायता”से करें। यह राशि केंद्र सरकार से मिलने वाली पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सहायता का 40 प्रतिशत है। यह वित्तीय सहायता तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश के 50 प्रतिशत कैपेक्स मदद से कम है, और असम के 40 प्रतिशत कैपेक्स के बराबर है। लेकिन यह साफ़ है कि केवल वित्तीय प्रोत्साहन ही किसी राज्य को निवेश के लिए आकर्षक नहीं बना देते। कर्नाटक ने तो 2022 में सेमीकंडक्टर कंपनी टॉवर सेमीकंडक्टर और कुछ दूसरी कंपनियों के एक कंसोर्शियम (जिसे ISMC कहा जाता है) के साथ एक करार पत्र पर दस्तखत किए थे, लेकिन $3 अरब का प्रस्तावित निवेश साकार नहीं हो पाया।
नए इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल्स बनाने पर सीमित ध्यान
सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और उसकी जटिलता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जो प्रौद्योगिकी के विस्तार या इंटीग्रेशन के साथ-साथ ताक़त, प्रदर्शन, विश्वसनीयता और सुरक्षा की बढ़ती मांगों से प्रेरित है। इस बारे में सोचा जाना चाहिए कि क्या सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में एक नया वर्टिकल बनाने का मौका है, जैसे मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल्स को आसान बनाना, जो फिलहाल सिर्फ़ तीन अमेरिकी कंपनियां बनाती हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि लागत संबंधी चुनौतियों का हल निकालने या बाज़ार की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल की नई परिस्थितियां विकसित करने की काबिलियत उद्योग में है।
साथ ही, नए बाज़ारों के खुलने से सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में इनोवेशन भी हुए हैं। यह लगातार चलने वाला और कभी न खत्म होने वाला एक चक्र है, जैसा कि क्वालकॉम के मामले में देखा जा सकता है। जब मोबाइल फ़ोन बाज़ार में आए, तो हैंडसेट बनाने वाली कंपनियां ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने में जी-जान से लगी थीं जिससे लोग हैंडसेट के ज़रिए एक-दूसरे से बात कर सकें। क्वालकॉम ने बहुत जल्दी यह समझ लिया था कि चिप्स का आकार घटने से ज़्यादा कम्प्यूटिंग पावर मिलेगी और इसका नतीजा यह होगा कि अलग-अलग फ़्रीक्वेंसी के बीच कॉल डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर हासिल हो सकेगी (इसके विपरीत कि बाकी कंपनियां एक ही फ़्रीक्वेंसी पर कॉल डेटा ट्रांसमिट करने के सिस्टम का प्रस्ताव रख रही थीं)। इस आइडिया को लागू करने के लिए क्वालकॉम ने ज़रूरी तकनीकी ढांचा तैयार किया। नतीजा यह हुआ कि क्वालकॉम ने स्पेशलाइज़्ड चिप्स पर अहम टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक पेटेंट कराया जो अलग-अलग फ़्रीक्वेंसी पर कॉम्प्लेक्स सिग्नल की व्याख्या कर सकती थीं।1 यह एक उदाहरण है कि कैसे नए बाज़ारों ने चिप डिज़ाइन में इनोवेशन को बढ़ावा दिया। इससे हम इस बिंदु तक पहुंचते हैं कि कुछ नए बाज़ारों की तलाश की जा सकती है, और उन बाज़ारों में, कैसे नई डिवाइस बनाई जा सकती हैं।
नए एंड-प्रोडक्ट्स के लिए बौद्धिक संपदा बनाने पर फोकस
इसलिए, यह सोचना फायदेमंद होगा कि क्या भारतीय कंपनियां अगली पीढ़ी के तकनीकी उपकरणों पर काम कर सकती हैं, जिनकी ज़रूरत करीब 10 साल बाद पड़ सकती है, और जहां अभी तक कोई देश अग्रणी नहीं बना है। यह कहना अक्सर अप्रासंगिक हो जाता है कि दुनिया भर में चिप डिज़ाइन करने वाले 20 फीसदी लोग भारत में काम करते हैं। लेकिन ये लोग ज़्यादातर ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनियों के बताए गए निर्देशों पर काम करते हैं। भारत में अपनी खुद की बौद्धिक संपदा बनाना और उसका मालिकाना हक हासिल करना अभी भी एक चुनौती है। भले ही सेमीकंडक्टर के मैच्योर नोड्स बनाना भी बाज़ार की ज़रूरतें पूरी करता है, फिर भी ध्यान उन्नत उपकरणों के विकास पर होना चाहिए, जैसे कि मेडिकल डायग्नोस्टिक के फील्ड में। मेडिकल डायग्नोस्टिक डिवाइसेज़ में सेंसर का इस्तेमाल करने वाली मशीनें, अल्ट्रासाउंड तकनीक का इस्तेमाल करने वाली इमेजिंग तकनीक, और न्यूरल इंटरफ़ेस तकनीक (जैसा कि न्यूरालिंक जैसे नए उपकरणों में देखा गया है) शामिल हैं।
इन उपकरणों से इकट्ठा किए गए डेटा को समझने और उसका विश्लेषण करने की भी ज़रूरत होगी, जैसे कि कोई डायग्नोस्टिक सुझाना या किसी तकनीशियन से सही जांच की सलाह देना। इसलिए अगली पीढ़ी की तकनीक पर शोध और विकास (R&D) में निवेश करना सही हो सकता है, जैसे टेक वेयरेबल्स और सॉफ़्टवेयर का इंटीग्रेशन। भले ही यह काम सीधे तौर पर ISM का नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी औद्योगिक नीति से जुड़ा मुद्दा है, फिर भी, इसे सेंटर फ़ॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की तरफ से चलाए जा रहे डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के साथ मिलाकर देखा जाना चाहिए।
निष्कर्ष
भारत का सेमीकंडक्टर मिशन अभी तक कामयाब रहा है। 10 अरब डॉलर के फंड के साथ, जिसका कुछ हिस्सा शायद अभी इस्तेमाल होना बाकी है, ISM ने सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के हर स्टेज से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए संसाधनों को सही ढंग से पहुंचाने का सराहनीय काम किया है। एक मज़बूत सप्लाई चेन बनाने का मतलब यही होता है। लक्ष्य यह नहीं था कि पूरे इकोसिस्टम का हर हिस्सा पूरी तरह यहां तैयार हो, बल्कि इतना मज़बूत बनाया जाए कि सप्लाई चेन टिकाऊ रहे। यह देखते हुए कि भारत ने सिर्फ 4 साल पहले एकदम शून्य से शुरुआत की थी और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन जैसी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री में काम किया, मौजूदा प्रयास अच्छी तरह लागू किए गए हैं। आगे चुनौतियां ज़रूर हैं, चाहे सप्लाई चेन को भारत के अलग-अलग हिस्सों तक फैलाना हो या फिर वैल्यू चेन में और ऊंचाई हासिल करना हो। लेकिन आज चुने गए रास्ते भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा के भविष्य के लिए शुभ संकेत देते हैं।